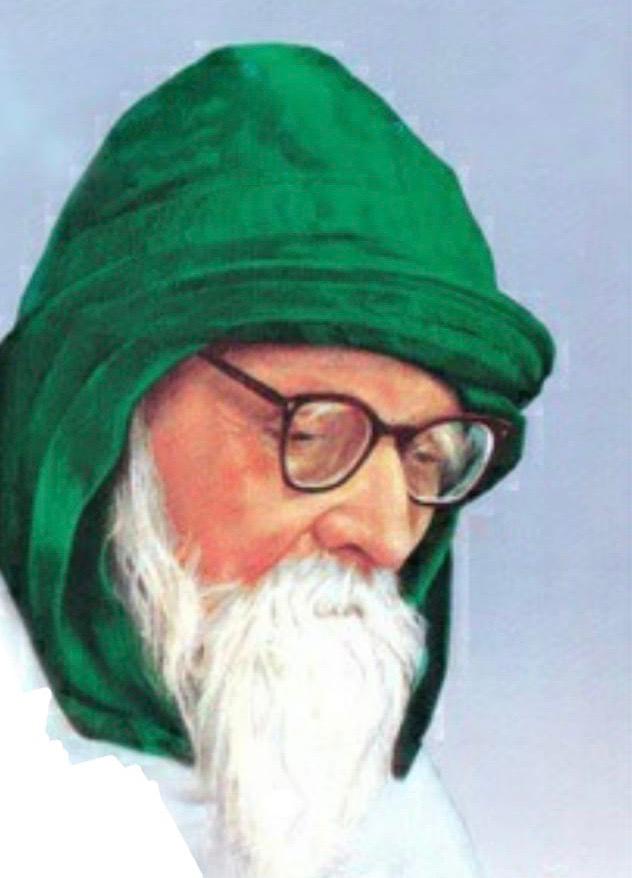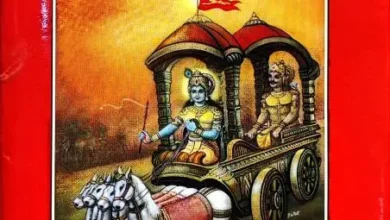मुक्ति के लिए कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं
आज का वेद चिंतन विचार

ईशावास्य उपनिषद जिजीविषेत् शतं समाः – जिजीविषा यानी जीने की इच्छा।
समाः शब्द संवत्सर का पुराना रूप है। सौ साल जीना है- उसमें उत्साह भी बताया है और मर्यादा भी। वैसे सामान्यतः आयु 60-70 साल की मानी जायेगी।
सतयुग में 500 साल, त्रेता में 300 साल, द्वापर में 200 और कलियुग में आयुर्मर्यादा 100 साल की मानी गयी है।
वैसे तो मनुष्य का जीवन परमेश्वर की इच्छा से ही चलता है। इसलिए सौ साल जीना या पचास साल जीना, यह मनुष्य के हाथ की बात नहीं है।
किंतु मनुष्य देह की मर्यादा सौ साल मानकर सौ साल जीने की चाह रखें, ऐसा आदेश यहां शास्त्रकारों ने दिया है।
सामान्यतः सौ साल की मर्यादा को पहुंचना कठिन नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीवन योग्य तरह से जीना सीखना होगा।
बाकी समत्वप्राप्त मनुष्य को मरण की या जीवन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
कुल नरसमूह को लक्ष्य करके सौ साल जीने की यह बात कही गयी है। वह साधक या कुछ विशेष लोगों की ही बात नहीं है।
‘सौ साल जीने की इच्छा रखे‘, अर्थात् कर्म करते-करते ही। इसलिए आरोग्य की उपेक्षा न करें, समत्वयुक्त जीवन जीयें, मानसिक क्षोभ न होने दें।
उसके कारण शक्तिक्षय होता है। शक्तिक्षय के सब दरवाजे बंद करने चाहिए।
जिजीविषेत् शतं समाः– यह वाक्य शंकराचार्य को भी थोड़ा कठिन गया है।
उस पर भाष्य करते हुए उन्होने कहा है- यो हि जिजीविषेत् स कर्म कुर्वन्। जिसके मंन में यह होगा कि कर्म करना अभी शेष है, उसे कर्म करते-करते जीना चाहिए।
कर्म करना शेष है, ऐसा न लगता हो तो जीने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जीने की इच्छा करना अज्ञान का लक्षण है।
आगे कहा है कि ईशावास्य का यह मंत्र ज्ञानी मनुष्य के लिए नहीं है, अज्ञानी मनुष्य के लिए है।
ईशावास्य का पहला मंत्र ज्ञानी पुरूष को लागू होता है। दूसरा, सामान्य साधक को लागू होता है।
और इन दोनों से भिन्न, जो नरकभाजक है, उस मनुष्य को तीसरा मंत्र लागू होता है।
ज्ञानी, साधक और नरक में जाने वाले पापी, तीनों को ध्यान में रखकर उन्होंने यह विवेचन किया है।
एंव त्वयि – तेरे लिए यही एक रास्ता है।
न अन्यथा इतः अस्ति – दूसरा रास्ता है ही नहीं।
न कर्म लिप्यते नरे – मनुष्य को कर्म का लेप नहीं होता।
देहधारी मनुष्य, देह है तब तक निष्काम सेवा करता जाये, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। देह में अनेक इंद्रियां हैं, उनसे निंरतर काम लेना, कर्मयोग है।
शरीर है तो उससे समाज को कुछ सेवा मिलनी चाहिए। अगर देह नहीं होती, तो फिर चिंतन से भी काम चल जाता ।
साधकावस्था में कर्ममुक्ति की बात करना गलत है। ज्ञान की अंतिम अवस्था में कर्ममुक्ति की बात हो सकती है।
साधकावस्था में, विषयवासनामुक्ति
सिद्धावस्था में, कर्ममुक्ति
साक्षात्कार की अवस्था में, देहमुक्ति
अक्सर कहा जाता है कि साधक को कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका लेप होता है। मनुष्य को कर्म चिपकता नहीं, वासना चिपकती है।
ऋषियों ने कर्म को रोड़ा समझकर मुक्ति के लिए कर्म छोड़़ने के कई प्रयोग किये और फिर अपना अनुभव दुनिया को बताते हुए कहा कि मुक्ति के लिए कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है।
देह के साथ कर्म तो आता ही है। परन्तु फल की वासना मनुष्य को सताती रहती है। इसलिए फलवासना को काटकर, अनासक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए।
कर्मफल की वासना मनुष्य के चित्त पर असर करती है जिसके कारण हम बंधन में पड़ जाते हैं।
उस वासना को काटकर कर्म किया जाये तो फिर कर्म का लेप नहीं होता। अलावा, केवल बाहर से कर्म छोड़ देने से कर्म छूटता नहीं।
बाहर से कर्म छोड़ दें , लेकिन अन्दर से वासना रखें तो वह भयंकर हो जायेगा। उस मनुष्य का जीवन पराक्रमी नहीं होगा।
मनुष्य का पराक्रम इसमें है कि वह वासना काटे। फिर कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं। काम करने से आत्मा को कोई बंधन नहीं होता, आत्मा को फलवासना की बाधा होती है।
वासना तोड़ने के लिए ज्ञान ही साधन हो सकता है। वासना को आत्मज्ञान से तोड़े। हमें यही करना है कि ज्ञान से वासना तोड़ते जायें और निष्काम कर्म करते जायें।
तो समझने की बात है कि मनुष्य को कर्म का लेप नहीं होता। कर्म तब बंधनरूप होता है जब हम कर्म के अंहकार से अपने को बांधते हैं।