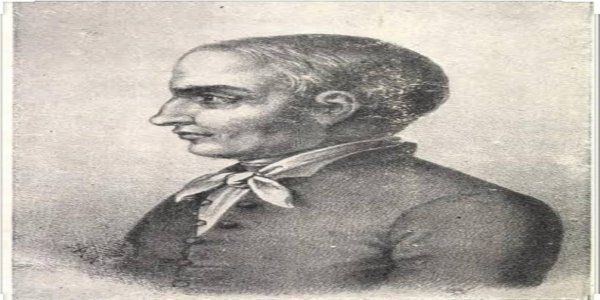और भारत खोजी चोमा पहुंच गये लद्दाख

त्रिलोक दीप
अलेक्जांडर चोमा द कोरोश के बारे में कुछ विद्वानों से भी बातचीत हुई थी। सांसद हीरेन्द्र नाथ मुखर्जी (जिन्हें प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी के तौर पर भी जाना जाता है), सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय और प्रोफेसर लोकेश चंद्र भी चोमा को न केवल विलक्षण प्रतिभा का धनी मानते थे बल्कि एक ऐसा बहुआयामी भाषाविद और धुनी यूरोपीय जो न उनसे पहले कोई पैदा हुआ था और न ही शायद उनके बाद होगा। उनके लिए तपस्वी और साधक की संज्ञाओं का प्रयोग भी किया जाता है।

हीरेन मुखर्जी का मानना है कि वह जुनूनी थे, सनकी या झक्की नहीं थे। जब उन्होंने एक बार ठान लिया कि अपने पुरखों की मूलभूमि तलाश करके रहूंगा तो न तो उनके भाईबंधु और न ही मित्र प्रोफेसर उन्हें अपने इरादे से डिगा सके। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चोमा महज एक झोले और छड़ी लेकर निकल पड़े थे। ऐसा लगता है कि पैदल चलते हुए रास्ते में आने वाली दिक्कतों का उन्हें एहसास नहीं था। क्या वे भगवान बुद्ध थे जिनकी तपस्या को देखकर कोई देवदूत उनसे वर मांगने को कहेगा या वे गुरु नानक थे जो सिर्फ अपने दो शिष्यों के साथ पैदल आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे?
माना जाता है कि बुद्ध और गुरु नानक दोनों के पास अलौकिक शक्तियां भी थीं। चोमा के पास क्या था ? दृढ़ निश्चय, संकल्प और इच्छा शक्ति, जुझारूपन, जज्बा, ईमानदारी तथा समर्पित प्रयास। क्या इन गुणों के साथ किसी मंज़िल को पाया जा सकता है, यह विचारणीय था।
उनके पास विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र , थोड़े से पैसे औऱ पहनने के लिए मामूली से कपड़े थे। उन्होंने अपनी मंशा साफ करते हुए भारतविद जेम्स प्रिंसेप को पत्र लिखकर कहा था कि मुझे सरकार किसी तरह की राजनीतिक जानकारियां लेने नहीं भेज रही है और मैं खुद भी इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं कहीं किसी तरह के आंकड़े, राजनीतिक या कोई भौगोलिक जांच पड़ताल से अपने आप को अलग रखूं। वे इतने सतर्क रहते थे कि अंग्रेज़ी समाचारपत्रों को भी हाथ नहीं लगाते थे, ताकि कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाये और उनका अपना ध्यान मुख्य मुद्दे से न भटक जाये। अपनी निजी आदतों के मामले में भी चोमा बहुत सावधानी बरता करते थे ।
प्रोफ़ेसर हीरेन मुखर्जी को मैं अपने लोकसभा सचिवालय की नौकरी (1956-65) के दिनों से ही जानता था। उनसे मिलता भी रहता था। उनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से था लेकिन विद्वान होने के कारण सभी दलों में उनकी बहुत इज़्ज़त थी। जब भी वह किसी विषय पर बोलते तो पूरी तैयारी के साथ। उन्हें सुनने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद आतुर रहते, यहां तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सदन में मौजूद रहते थे।
लोकसभा छोड़ने के बाद भी प्रोफ़ेसर मुखर्जी से मेरा संपर्क बना रहा। ‘दिनमान’ के लिए कई मुलाक़ातें हुआ करती थीं। हंगरी पर अपनी एक पुस्तक भी उन्होंने मुझे भेंट की थी। उन्होंने बुडापेस्ट की एकेडमी ऑफ साइंसेज में बैठ कर चोमा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। लिहाज़ा जब मैं कभी चोमा पर बात करता तो वह अतीत में खो जाते और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। यह पोस्ट लिखते हुए सहसा उनकी याद हो आयी। उन्होंने बताया था कि अनुभवों के थपेड़ों को झेलते हुए जब चोमा अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो गये तब कश्मीर में उनकी मुलाकात ब्रितानी अन्वेषक और खोजी मूरक्राफ्ट से हो गयी। चोमा को मूरक्राफ्ट के रूप में शायद पहला ऐसा इंसान मिला जिसके सामने अपने मन की व्यथा का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे बताया था। दोनों में दोस्ती हो गयी और वे एक साथ लेह पहुंच गये। मूरक्राफ्ट ने चोमा को तिब्बत की एक वर्णमाला देते हुए यह कह कर उत्साहित किया कि आप अपने फ़ारसी के ज्ञान का इस्तेमाल तिब्बती सीखने में करो।
इसके लिए उन्होंने जांस्कर के जांगला के लामा विद्वान की सेवाओं का भी प्रबंध कर दिया। उस लामा के साथ रहकर चोमा ने न केवल तिब्बती का अध्ययन किया बल्कि कई मठों में संग्रहीत नायाब साहित्यिक खज़ाना उनके हाथ लगा। अब चोमा का मन तिब्बत और तिब्बती में रमने लगा। मूरक्राफ्ट ने कई लोगों के नाम व परिचय पत्र दिये और साथ में कुछ पूंजी भी। मूरक्राफ्ट की इस सहायता के एवज में चोमा को तिब्बती-अंग्रेज़ी शब्दकोश और तिब्बती व्याकरण तैयार कर सरकार को देनी थी। चोमा ने शर्त मंज़ूर कर ली। लेकिन लामा अचानक कहीं गायब हो गया और चोमा को मंझधार में छोड़ गया। चोमा न तो हताश हुए और न ही निराश। इसे वे अपनी फितरत मानते थे।
यह भी संयोग देखिये जिस साल 1784 में चोमा का जन्म हुआ उसी बरस कलकत्ता (अब कोलकाता) में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इस सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोंस जो अपने समय के महान मानवतावादी और प्रसिद्ध ब्रितानी प्राच्यविद थे। काफी समय बाद चोमा उनसे जुड़े। वहां तक पहुंचने में चोमा को कई दुश्वारियों से गुजरना पड़ा। उस लामा के गायब हो जाने के बाद तीर्थयात्री विद्वान चोमा एक बार फिर ऊहापोह की स्थिति में पड़ गये। मूरक्राफ्ट का निधन हो चुका था, कैप्टेन कैनेडी जो उनके प्रति हमदर्दी रखते थे, वे विद्वान नहीं थे, इसलिए उनके मुश्किलात को समझ नहीं सकते थे। कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी उनके, तिब्बती भाषा और साहित्य के बारे में शायद ही कुछ जानती हो।
इस असमंजस के बावजूद उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर यह निवेदन किया कि या तो उन्हें कलकत्ता जाकर अपनी स्थिति से अवगत कराने का अवसर दिया जाये अथवा तिब्बत में तीन बरस और रहकर अपना अध्ययन कार्य पूरा करने का मौका दिया जाये । सन् 1827 की बसंत को चोमा को गवर्नर जनरल लार्ड एमहर्स्ट के समक्ष पेश होने को कहा गया जहां उन्होंने स्थिति बयान की।
चोमा के आत्मविश्वास से लबरेज़ अंदाज़ और विद्वत कार्य से गवर्नर जनरल बहुत प्रभावित हुए और उन्हें न केवल तीन साल के लिए तिब्बत में रहने की अनुमति ही दी बल्कि पचास रुपये प्रति मास का भत्ता भी बांध दिया।
चोमा बेशक़ विस्मत कर देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पहाड़ों की कठोर और प्रतिकूल जलवायु के बीच रहते हुए तिब्बती पांडुलिपियों का बहुत बड़ा और समृद्ध खज़ाना तैयार कर लिया था। जिस तरह कठोर जलवायु में बिना अधिक खाये पिये अपने काम को चोमा ने अंजाम दिया आम यूरोपीय के लिये ऐसी स्थिति में रहना न केवल मुश्किल बल्कि असंभव था। दिलचस्प बात यह थी कि चोमा ने उन पचास रुपयों में से बमुश्किल पंद्रह रुपये ही माहवार खर्च किया होगा। और इस प्रकार उन्होंने करीब पांच सौ रुपये बचा लिये थे। प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी चोमा के बारे में बताने में इस क़दर मशगूल हो गये मानो वे खुद उनके साथ हों। वादे के मुताबिक तीन बरस तक तिब्बत की पहाड़ियों के शिखर पर लगातार बैठ कर 26 मार्च, 1830 को चोमा ने अपना लेखन कार्य पूरा कर लिया जिसे कैप्टेन कैनेडी ने अनुकरणीय बताया। उन्होंने सरकार से चोमा की कलकत्ता यात्रा तथा साथ में उनकी पुस्तकों तथा पांडुलिपियों को ले जाने के लिये पांच सौ रुपये स्वीकृत करने की सिफारिश की जो तुरन्त मिल गई।
अप्रैल, 1931 को चोमा अपने बहुमूल्य सामान के साथ कलकत्ता पहुंच गये और 5 मई, 1831 को सरकार के सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। शब्दकोश की प्रस्तावना में चोमा ने लिखा कि ‘विधि का शायद ऐसा ही विधान था जो मूरक्राफ्ट की सहायता से मुझे तिब्बत ले गया और मैं बाखुशी तिब्बती साहित्य के अध्ययन में रम गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद यही मेरे उद्देश्य का वाहक सिद्ध हो । मेरा तात्पर्य हंगेरी मूल और उसकी भाषा के अनुसंधान से है ,जिस मकसद को लेकर मैं अपने देश से पैदल निकला था।’
सन् 1834 से 1837 तक वे एशियाटिक सोसाइटी के मानद सदस्य रहे जिसे उस जमाने में एक असाधारण सम्मान माना जाता था। वहां रहते हुए चोमा ने शब्दकोश और व्याकरण को छपवाने की व्यवस्था की। उन्होंने तिब्बती शब्दावली का अनुवाद कराया जिसे बुद्ध प्रणाली एवं व्यवस्था का सारांश माना जाता है। कुछ पृष्ठों की लिथोग्राफी हुई, अधिकांश की टाइपोग्राफी तथा कुछ के रेखांकन तैयार हुए।
चोमा ने इन ग्रंथों की पचास प्रतियां हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेज को भी भिजवाई, जिनका भुगतान उन्होंने अपनी बचत से किया। तब तक लार्ड एमहर्स्ट के स्थान पर लार्ड विलियम बैंटिक नये गवर्नर जनरल बन कर आये जिन्हें इस ‘विलक्षण तीर्थयात्री विद्वान ‘ के बारे में जानकारी दे दी गयी।
चोमा द कोरोश संस्कृत और उसकी सखी भाषाओं को मांजने के काम में जुट गये। उनका मानना था कि भाषाशास्त्र और उस से संलग्न भाषाओं का ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक संस्कृत पर पूरी तरह से मास्टरी न हो। इस सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जेम्स प्रिंसेप से दो पासपोर्ट बनवाने को कहा। चोमा का मकसद उत्तर पूर्व बंगाल के अलावा भारत के उत्तर पश्चिम भाग की भी यात्रा करना था। एक पासपोर्ट उनके अंग्रेज़ी नाम यानी ‘मिस्टर अलेक्जांडर चोमा, हंगेरी दार्शनिक, ट्रांसिलवनिया निवासी’ के नाम पर था और दूसरा उनके फ़ारसी नाम पर था अर्थात ‘मौला इस्कंदर चोमा अज़ मुल्क-इ-रूम’। उन्होंने अपनी तरफ से यह घोषणा भी कर दी कि किसी भी तरह की गुप्तचरी से न कोई वास्ता है और न ही उससे कुछ लेना देना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वह सरकार के माध्यम से यूरोप में लैटिन भाषा मे पत्र व्यवहार करेंगे और उनके सभी पत्र खुले होंगे, बन्द नहीं किये जायेंगे। चोमा ने अपने हर माह के पचास रुपये भत्ते को जारी रखने के लिए कहा। यह बात अलग है कि एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के लिये’ ‘बुद्ध साहित्य ‘ पर उन्होंने जो लिखा था उसका मेहनताना भी बनता था। चोमा को पासपोर्ट मिल गये और वे एक नाव द्वारा कलकत्ता से निकल कर गंगा नदी से उत्तरी बंगाल के मालदा में 20 जनवरी, 1836 को पहुंच गये। मालदा पहुंच कर उन्होंने प्रिंसेप को लिखा कि बिना किसी परेशानी के मालदा पहुंच गया हूं। रास्ते में खर्च का हिसाब भी पाई दर पाई लिख कर दे दिया। वहां ब्रितानी अफसर मेजर लॉयड ने चोमा की मेजबानी करनी चाही लेकिन उन्होंने सधन्यवाद मना कर दिया और एक झोपड़ी में डेरा जमाया तथा उबले चावल और चाय पर गुज़र बसर करने लगे। मेजर लॉयड ने चोमा की खिदमत के लिए एक सेवक का प्रबंध कर दिया। यही मेजर लॉयड दार्जीलिंग के संस्थापक माने जाते हैं। चोमा संस्कृत और बांग्ला के साथ-साथ वहां की स्थानीय बोलियों और उपभाषाओं का ज्ञान भी अर्जित करना चाह रहे थे। बिहार और बंगाल सीमा पर मैथिली भी वह इसीलिये सीख रहे थे कि उसका साहित्य बहुत सम्पन्न है। लेकिन मेजर लॉयड के मुताबिक चोमा संस्कृत और बांग्ला के अतिरिक्त मराठी का अध्ययन भी बड़ी गंभीरता से कर रहे थे। जनवरी, 1837 को संस्कृत भाषा का विद्वान बनकर चोमा कलकत्ता वापस लौट आये और एशियाटिक सोसाइटी के काम में जुट गये।
उन्हें सब-लाइब्रेरियन का पद और एशियाटिक सोसाइटी की बिल्डिंग में रहने का स्थान मिल गया। इतने प्रतिभशाली व्यक्ति की गरिमा के लिहाज से बेशक़ उन्हें किसी पद से न नवाजा जाता, अगर उनके लिए कोई पद तय करना ही था तो उनकी विद्वता के अनुकूल होना चाहिये था। चोमा तो बडे-बड़े पदों को ठोकर मार चुके थे। उन्होंने तो शायद अपने इस नये नामकरण की तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। एक छोटे से कमरे में अपने चारों ओर किताबों के चार बक्से रख कर बीच में चटाई बिछा ली। वहीं वह बैठते, काम करते और सो जाया करते थे। बेहतर हो उसे कमरा न कह कर कक्ष कहा जाये। वह शायद ही कभी अपने इस कक्ष से बाहर निकलते हों सिवाय कभी – कभी बिल्डिंग के बरामदे में थोड़ी देर चहलकदमी करने के लिये। वह अपने काम और विचारों में ऐसे खोये रहते थे कि अपने डेस्क पर लिखते-लिखते स्वयं ही हंसने लगते थे। हिमालय के मठों से उन्होंने इतनी बेशकीमती साहित्यिक और गूढ़लिपि पूंजी बहुरूप के तौर पर पाई थी, जिसके अर्थ निकालने और उनका वर्णन करने का सामर्थ्य चोमा के सिवाय किसी और में शायद ही था। किसी दूसरे यूरोपीय में तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो वे अपने कक्ष में बाहर से ताला लगवा दिया करते थे।
एशियाटिक सोसाइटी में कई बरसों तक सचिव रहे डॉ.मालान का कहना था कि चोमा एक अलग किस्म के इंसान थे जो बहुत ही विनम्र, कृपालु और दयावान थे। मध्यम कद के चोमा हर वह चीज़ आपसे साझा करने को तैयार हो जाते जो और जितना कुछ वह जानते थे। उनके साथ बैठ कर अदभुत आनंद का अनुभव होता था। डॉ.मालान ने कहीं लिखा है कि चोमा ने उन्हें सभी तिब्बती पुस्तकें दे दीं जो उन्होंने बाद में हंगेरी एकेडमी ऑफ साइंसेज को भेंट कर दीं।
चोमा अपने आप में इतने मगन रहते थे कि शायद ही कोई उनसे मिलने की जुर्रत कर पाता हो। सन् 1837 से 1842 के प्रारंभ तक वह एशियाटिक सोसाइटी के लिये अपनी पांडुलिपियोंऔर दूसरे ठोस कामों के सूचीकरण के काम में जुटे रहे। बीच-बीच में उन्हें अपने घर और देश की बहुत याद आया करती थी। अगर कोई उनसे हंगरी के बारे में बातें करता तो उसे बड़े शौक और चाव से सुन कर हंसते भी थे।
आखिरकार चोमा द कोरोश ने अपनी आत्मनिर्धारित ‘जेल ज़िंदगी’ से बाहर निकल खुली हवा लेने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि एक बार फिर पहाड़ों की ओर रुख कर अपने मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। 9 फरवरी, 1842 को उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को दिये गये अपने विदाई संदेश में अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी हर तरह की सहायता के लिए आभार जताया।
उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को यह भी सूचित किया कि अब वे मध्य एशिया की यात्रा पर जाने का इरादा रखते हैं और उनकी अनुपस्थिति में यूरोप से उनके नाम सोसाइटी में कोई पत्र आये तो उसका उत्तर जैसा वह उचित समझें दें। अपने पहले के संकल्प की पुनरावृति करते हुए चोमा ने लिखा कि अगर इस दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उनकी सभी चीजों और सामान पर एशियाटिक सोसाइटी का हक़ होगा। एक बार फिर चोमा ‘स्थानीय नाव’ से गंगा नदी से उत्तर की ओर निकल पड़े। उसके बाद पैदल ही ‘तराई’ से होते हुए पहाड़ियों की तरफ हो लिये। वह दलदली ज़मीन थी जिसे ‘मृत्यु-जाल’ माना जाता था, खास तौर पर यूरोपीय लोगों के लिये वह मलेरिया बुखार के गढ़ के रूप में देखा जाता था। चोमा को इस बाबत चेतावनी भी दी गयी लेकिन हंगरी से पैदल चल कर भारत पहुंचने वाला चोमा अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त थे। धीरे-धीरे पैदल चलते हुए वे 24 मार्च को दार्जीलिंग पहुंच गये। लेकिन 6 अप्रैल को वे मलेरिया के काबू में आ गये। दार्जीलिंग स्थित मुख्य अधिकारी डॉ. कैम्पबेल ने चोमा का उपचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।चोमा बार – बार मध्य एशिया जाने की बातें करते लेकिन डॉ. कैम्पबेल जानते थे कि चोमा की इहलीला कभी भी समाप्त हो सकती है। चोमा कहते थे कि यूरोप के लोग क्या सोचेंगे कि मैं उनकी मूलभूमि का पता लगाने के लिए ल्हासा नहीं जा सका।
जब चोमा को अपना अंत नज़दीक आते हुए दिखाई दिया तो उन्होंने अपना सारा सामान, किताबें, नकदी डॉ.कैम्पबेल के सुपुर्द कर दिया। 11 अप्रैल, 1842 की सुबह 5 बजे चोमा का निधन हो गया। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए डॉ.कैम्पबेल ने चोमा का सारा सामान जिसमें किताबों और दस्तावेज़ों के चार बक्से, नीले रंग का सूट जो चोमा ने पहन रखा था, कुछ शीट्स और एक कुकिंग पॉट, 300 रुपए के बैंक नोट, 5 हज़ार रुपये की बाबत सरकार के नाम एक ज्ञापन, 224 रुपये के सिक्के , और एक कमरबन्द जिस में 26 स्वर्णमुद्राएँ थीं एशियाटिक सोसाइटी के सुपुर्द कीं ।
अपने पीछे चोमा जो संपन्न विरासत छोड़ गये हैं वे केवल हंगरी या यूरोप के लिये ही नहीं पूरे विश्व के लिये एक अद्भुत देन है। किसी ने चोमा को अपनी श्रद्धांजलि कुछ इस प्रकार दी है – हिमालय के शिखर पर एक ऐसा संत तीर्थयात्री विद्वान दफन है जहां उल्का चलचित्र निर्मित करते हैं, बादल उमड़ते घुमड़ते कई आकार लेते हैं, जहां बिजली अपनी गर्जना भूल कर विनीत बन जाती है तथा सितारे कभी आते हैं , कभी जाते हैं, मानो वहां चिर निद्रा में सोये महामानव को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हों।
चोमा के बारे में बोलते हुए हीरेन मुखर्जी कहते थे कि वह कोई अटकलबाज नहीं थे बल्कि वह ऐसे वैज्ञानिक-अनुसंधानकर्ता थे जिन्हें अपने अध्ययन की व्यावहारिकता के साथ- साथ विश्लेषण का भी इल्म था। उन्होंने दुनिया के सामने तिब्बती ज्ञान भंडार के अगुआ का काम किया और यूरोप में बौद्ध अध्ययन को और विस्तृत किया।
यह पूछे जाने पर कि क्या किसी और हंगेरी या यूरोपीय ने चोमा का रास्ता अपनाया, प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने बताया कि चोमा के देहांत के 24 बरस बाद , एक उनके ही देशवासी विद्वान जी. डब्ल्यू. लेइटनेर ने 1866 में लद्दाख यात्रा के दौरान फुकटल मोनेस्ट्री यानी मठ का अवलोकन किया। वहां के मठाधीश ने मठ के वे सारे स्थान उन्हें दिखाये जहां चोमा रहते और काम किया करते थे। मठाधीश के अनुसार चोमा को लोग बहुत स्नेह करते थे और सम्मान भी देते थे। प्यार से उन्हें वहां के लोग ‘फिलेंगी दास ‘ यानी विदेशी शिष्य कहते थे। उनकी निःस्वार्थ भावना, बिना किसी के गिला शिकवा, सहनशीलता, अनंत विनम्रता, अथक परिश्रम जैसे गुणों ने यहां के लोगों को बहुत प्रभावित किया था।
जब लोगों को यह पता चला कि लेइटनेर भी चोमा के देश से आये हैं तो मठाधीश ने उन्हें विशेष सम्मान देते हुए उनके समक्ष एक अभूतपूर्व प्रस्ताव रखा।
मठाधीश ने कहा कि यदि वह ल्हासा जाना चाहते हैं तो उनके आने – जाने का प्रबंध किया जा सकता है । उनकी सुरक्षा के लिए अगर सरकार को कोई गारंटी चाहिए तो वह खुद अपने दो बेटों को सरकार के पास बंधक रखने को भी तैयार हैं। मठाधीश का यह खुला निमंत्रण था कि अगर लेइटनेर इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो वह चोमा से प्रेम और तिब्बत तथा तिब्बती के प्रति उनके समर्पण की भावना को देखते हुए किसी भी यूरोपीय के लिये यह खुला निमंत्रण है।
लेइटनेर ने बहुत से यूरोपीय विद्वानों से ल्हासा जाने के इस निमंत्रण पर बात की लेकिन कोई भी इस विस्मयकारी अवसर का लाभ उठाने को तैयार नहीं हुआ। उस मठाधीश को बार-बार चोमा की याद आ रही थी कि काश मैंने चोमा को यह प्रस्ताव दिया होता। तो वे न केवल बाखुशी इसे स्वीकार करते बल्कि मेरा कई बार आभार भी मानते। ल्हासा से जो वह नायाब सामग्री लाकर देते उससे विश्व में तिब्बती साहित्य की अभिवृद्धि में इज़ाफ़ा होता सो अलग।
हीरेन मुखर्जी का तर्क था कि शायद उनमें से किसी की भी चोमा जैसी साफ़ छवि नहीं थी।चोमा ने बिना किसी लागलपेट और स्वार्थ के अपने मन की आवाज़ सुन अपनी मूलभूमि खोजने का बीड़ा उठाया था। वे आत्मप्रेरित थे, किसी के सुझाव या दबाव का परिणाम नहीं थे।
हंगरी से पैदल चलकर अपनी मूलभूमि तक पहुंचने को आप क्या कहेंगे, जुनून ही न। न किसी से मदद ली, न किसी से पैसा लिया और जिस से लिया भी तो उसे सूद समेत वापस किया। है किसी में इतनी कुव्वत, दमखम? सदियों में कहीं ऐसे संत तीर्थयात्री विद्वान पैदा होते हैं। ऐसे थे चोमा! बेशक़।

इस दलील को आगे बढ़ाते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कहा था कि चोमा विश्व साहित्य को जितना संपन्न कर गये हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तिब्बती और संस्कृत में उनके योगदान पर चर्चा होती है, इस बात पर भी बातचीत की जाती है कि बौद्ध साहित्य में उनका कितना योगदान था लेकिन इस बात का कम ही उल्लेख होता है कि अन्य भाषाओं को चोमा के साहित्य की क्या और कितनी देन थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चोमा भाषाविद थे, गोएटिंग विश्विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की थी, जर्मन भाषा में भी उनकी मास्टरी थी। वैसे भी हंगरी में जर्मनी बोली जाती है। मेरा तो मानना है कि फ़्रेडरिक मैक्स म्युलर ने ऋग्वेद का अनुवाद जो किया था उसमें चोमा की साहित्यिक प्रतिभा का खासा योगदान था। वात्स्यायन जी के आकलन को गंभीरता से इस मायने में लिया जाना चाहिये कि वह हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर कई बार जा चुके थे। इसके अलावा कैलिफोर्निया की बर्कले विश्वविद्यालय में वह नियमित तौर पर अतिधि प्राध्यापक के तौर पर जाया करते थे। हाइडलबर्ग विश्विद्यालय में प्रोफ़ेसर लौठार लुत्से उनके करीबी मित्रों में थे। वह संस्कृत के विद्वान नहीं थे लेकिन अल्ब्रेखत वेबर, फ्रांज़ बेरनहार्ड, हेज़ बेचेखरत आदि संस्कृत और बौद्ध अध्ययन के सम्मानित हस्ताक्षर थे।
खुद मैक्स म्युलर ने भी यह माना है कि यूरोप में वैदिक, पाली और बौद्ध अध्ययन के प्रचार – प्रसार का श्रेय विस्मयकारी ‘तीर्थयात्री विद्वान’ को जाता है। उनके अध्ययन और पुस्तकों के कारण इन भाषाओं को बहुत अहमियत मिली है। बोन विश्वविद्यालय में तो एशियाटिक सोसाइटी ने’संस्कृत चेयर’ स्थापित कर रखी है। इसी प्रकार बर्कले में रहते हुए वात्स्यायन जी को यह भी पता चला अमेरिका और मेक्सिको में संस्कृत और पाली भाषा के कई विद्वान हैं जो चोमा के साहित्यिक ज़खीरे से परिचित हैं। वात्स्यायन जी को कई लोग यायावर भी कहते हैं। घुम्मकड़ तो वे शुरू से रहे ।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया था कि लद्दाख तो कई बार गया हूं, अविभाजित भारत के समय और बाद में भी। उन्होंने भी चोमा के परिश्रम और दिनरात काम करने के बारे में सुना था। वहां के हेमिस गुम्पा सहित कई गुम्पों में संग्रहीत बहुत से ग्रंथ देखे और पढ़े भी लेकिन जंस्कार नहीं जा सके जहां चोमा ने अध्ययन किया था।
राहुल सांस्कृत्यायन के ‘मध्य एशिया के इतिहास’ पर चोमा के प्रभाव पर उनका मानना था, असंभव नहीं। चोमा तिब्बती और संस्कृत का गंभीर अध्ययन कर जो साहित्य लिख गये थे उसमें मूल भाषा के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद भी शामिल था। अंग्रेज़ी सरकार को जो शब्दकोश और व्याकरण उन्होंने भेंट किये थे वे अंग्रेज़ी में ही थे। उनका इतना खज़ाना था जो अंग्रेज़ी के इतर भी था। नामुमकिन नहीं राहुल सांस्कृत्यायन जी ने चोमा के इस व्यापक साहित्य की सहायता ली हो।’ चोमा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 24 साल बाद उनके एक देशवासी लेइटनेर के फुकटल मठ जाकर चोमा के अध्ययन का आकलन करने की तो खबरें हैं लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उन जैसा काम करने वाले विद्वान का कहीं नाम सुनने को नहीं मिलता।
वात्स्यायन जी थोड़ा मुस्कराये और बोले,’चोमा जैसे खब्ती विरले ही होते हैं जो पैदल अपने देश से चल कर मूलभूमि तलाशने का जोखिम उठा सकें। वह व्यक्ति किसी खास सवारी से उस मठ तक पहुंचे होंगे और संभव है कुछ जांच पड़ताल कर रहे हों।’
वात्स्यायन जी ने बताया कि ये मठाधीश कम विद्वान और काबिल नहीं होते। हो सकता है मठाधीश उस व्यक्ति की मंशा समझ गया हो जिसके चलते उसने ल्हासा वाला सुझाव दे दिया हो। चोमा के जांगसा वाले लामा की विद्वता के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब चोमा को उसने अपने से अधिक काबिल और विद्वान समझा तो एक बार तो वह उन्हें गच्चा दे ही गया था। बाद में लौट आया और चोमा के समक्ष नतमस्तक हो गया।
चोमा के साहित्य का हंगेरी एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक सार-संक्षेप तैयार कराया था जिसका संपादन भारत में संस्कृत और तिब्बती के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर लोकेश चंद्र ने किया था। एक भेंट में प्रोफेसर लोकेश चंद्र ने बताया कि चोमा द कोरोश , जिसे ककरोशी भी कहते हैं,मध्य एशिया जाकर अपने पुरखों की मूलभूमि के लिए निकले थे लेकिन हालात ने उन्हें भारत पहुंचा दिया और यहां वे तिब्बती की पढ़ाई में संलग्न हो गये। तिब्बत से होते हुए मंगोल देश जाने की इच्छा से उन्होंने तिब्बती का अध्ययन किया। हंगरी की मूल जाति की खोज का स्वप्न लेकर आये थे परन्तु एक और ही सत्य खोज निकाला। वह था भारत की राजनीतिक और भौगोलिक परिधियों से बाहर संस्कृत साहित्य की थाती का भव्य विस्तार। उन्हीं दिनों राजा राममोहन राय ने समस्त भारतीय परंपराओं के विरुद्ध अभियान चला रखा था — 11 दिसंबर, 1823 को उन्होंने गवर्नर जनरल को पत्र लिखा जिसमें अंग्रेज़ी शिक्षा का घोर समर्थन किया। उसके विपरीत, प्रबुद्ध अंग्रेज न्यायाधीश और प्रशासक भारत के इतिहास और संस्कृत के अध्ययन में लगन से प्रवृत्त थे। 1829 में एशियाटिक सोसाइटी में प्रसन्नकुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और तीन अन्य भारतीयों को प्रथम बार सदस्य बनाया गया। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों में विचार मंथन चल रहा था। परंपरा और आधुनिकता में नये आयाम की खोज थी।
उन परिस्थितियों में कोरोशी का कलकत्ता के वातावरण में मौन परन्तु विलक्षण स्थान था। सन् 1834 में उनका तिब्बती व्याकरण और कोश प्रकाशित हुआ। तीन वर्ष तक (1834-37) उन्होंने संस्कृत का स्वाध्याय किया। सन् 1836 में उन्होंने कंजूर के ग्रंथों का विवरण प्रकाशित किया, जिसमें 1200 के लगभग संस्कृत की लुप्त कृतियों के तिब्बती भाषान्तर थे। पहली बार विश्व में भारत के अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वरूप का पता चला। हिमालय के अस्थिबेधी शीत में आधे भूखे, सिर से पैर तक कंबल ओढे, प्रातः से सायं हिमालय की गोद में ठिठुरते हुए, कोरोशी ने अदम्य उत्साह और अथक परिश्रम से, भारत के इतिहास में क्रांति कर दी। भारतीय इतिहास नयी दृष्टि से देदीप्यमान हुआ। जैसे यूरोप के लिए ग्रीस ज्योतिपुंज था, उसी प्रकार भारत एशिया के लिए काव्य और कला, दर्शन और विज्ञान का स्रोत बन गया। एशिया में भारत उनकी आत्मा और आलोक का प्रतीक बना। कोरोशी की तपस्या से भारतीय मानस में नये आत्मविश्वास का अभ्युदय हुआ।
प्रोफेसर लोकेश चंद्र ने आगे बताया कि एशियाटिक सोसाइटी में बैठे मौन साधक कोरोशी ने भारतीय मनीषियों की आत्मविस्मृति को झकझोरा और उनमें नयी आत्मचेतना का जागरण किया। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बंगाल में प्रारंभ हुआ। आगे चल कर ठाकुर परिवार भारत की नयी चेतना का अग्रदूत बना।
हंगरी के उदभव और अस्मिता के अन्वेषक कोरोशी ने भारत को आत्मविश्वास का मंत्र देकर दोनों देशों को एक सूत्र में पिरोया है। हमें विदित है कि भारत के अभ्युदय का विश्व कल्याण के प्रयास से अभिन्न नाता है। जहां कोरोशी हंगरी के राष्ट्रीय नेता के रूप में मानित, पूजित, वन्दित और नन्दित हैं, वे भारत के कालजयी स्वप्न को मूर्त बनाने के लिए पुकार रहे हैं। प्रोफेसर लोकेश चंद्र डॉ रघुवीर के पुत्र हैं, जिन्होंने सन् 1953 में संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने चीन और मंगोलिया की यात्रा कर तीसरी शताब्दी की संक्षिप्त रामायण, एक ध्वज जिस पर गायत्री मंत्र अंकित था, और बहुत से बहुमूल्य पुरावशेष एकत्र किये। उन दिनों विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता था। चीन की तिकड़ी फ़ा-हीएन, हिउन-त्सांग औऱ ई-तसिंग पांचवीं सदी में भारत-चीन सांस्कृतिक संबंध पुख्ता करने के कार्य में जुटे रहे, वह इसलिए भी क्योंकि सदा से भारत को ज्ञान की पाठशाला समझा जाता रहा है। बेशक़ चोमा की भारत की खोजी यात्रा से न केवल भारत की यूरोप में ही जय-जयकार हुई बल्कि विश्व के अन्य देशों में उसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक धाक भी जम गयी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और संडे मेल के पूर्व कार्यकारी संपादक हैं)