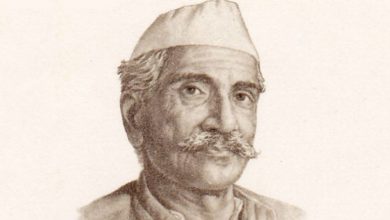गाँवों में कोरोना संक्रमण के साथ-साथ संघर्ष भी बढ़ रहा है।
 डॉ. चन्द्रशेखर प्राण
डॉ. चन्द्रशेखर प्राण
दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के शहरों से अपने गांव लौट रहे कामगार मजदूर, फुटकर व्यवसाई तथा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी जिन्हें “प्रवासी मजदूर” की संज्ञा दी गई है उनमें से एक बड़ी संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य से है। इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव में औसतन 40 से 50 कामगारों की वापसी हुई है। पिछले कुछ दिनों से संबंधित राज्यों में कोरोनावायरस की तेजी से बढ़ती हुई संख्या में इनका हिस्सा सर्वाधिक है। वास्तव में जिन शहरों में यह रह रहे थे वहां संक्रमण का प्रभाव तो अधिक था ही लेकिन जिस तरीके से यह आए हैं या लाए गए हैं उसमें भी उनके संक्रमित होने की काफी गुंजाइश थी। अब परिणाम सामने है।
इनके आगमन के साथ संबंधित क्षेत्र के गांव के जीवन में आशंका भय और दुख की स्थिति काफी चिंताजनक है। यह सही है कि यह अपने गांव आ रहे हैं , लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है इस महामारी ने परिवार के बीच में भी भय और दुराव की स्थिति पैदा कर दी है। गांव की बात तो अलग ही है।

गांव जो भारत के सामुदायिक समाज का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है वह समाज की विसंगतियों से इस कदर प्रभावित हुआ है कि उसके संबंधों में दरार तो आई ही है कहीं-कहीं तो चौड़ी और गहरी खाई भी बन गई है। ऐसे में बड़ी उम्मीदों के साथ शहर से भाग कर आए कामगारों को अपने गांव में पराएपन और विरोधी स्वर कुछ ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन सद्भाव और भाईचारे के स्वर भी हैं। जिसके उदाहरण भी बराबर मिल रहे हैं। समय ने सामाजिक संबंधों पर राख की मोटी परत जरूर चढ़ा दी है लेकिन अभी उसके अंदर की तपन मौजूद है जिसका एहसास इस संकट की घड़ी में रह-रहकर सामने आ रहा है।
राज्य सरकारों ने गांव लौट रहे लोगों के लिए एक निश्चित अवधि तक क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया है और स्थानीय स्तर पर इसकी जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को सौंपी है। ग्राम पंचायतों की स्थिति अधिकांश जगहों पर संतोषजनक नहीं है। इसके कई कारण है जिसमें ग्राम पंचायतों की क्षमता और सामर्थ्य की दृष्टि से कमजोर होना एक बड़ा कारण है।
सच्चाई तो यह है कि अधिकांश ग्राम पंचायतें अकेले प्रधान व मुखिया (ग्राम पंचायत अध्यक्ष) के सहारे टिकी है और वह भी उसे वे अपने हित-अहित के नजरिए से ज्यादा चलाते रहे हैं। कुछ गिने-चुने अध्यक्ष यदि उसे गांव के हित में चलाना भी चाहते हैं तो लोगों का अरुचि, उदासीनता, अविश्वास तथा साधनों का अभाव व सरकारी तंत्र की उपेक्षा के चलते वह भी कुछ ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।
दूसरी तरफ आने वाले ग्रामीणों में जो कमजोर वर्ग के हैं वह तो क्वारंटाइन सेंटर मैं रुकने को तैयार हो जाते हैं लेकिन जो सक्षम वर्ग के हैं वह उसके नियमों को ना मानकर अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। अब तो राज्य सरकारें भी इसे ही प्रोत्साहित कर रही हैं। वैसे स्वयं चलकर आए हुए लोग तो चोरी-छिपे अपने घरों में पहुंच ही जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण उनके परिवार से पड़ोस तक बड़ी तेजी से भी फैल रहा है।
गांव में संक्रमण के साथ-साथ संघर्ष भी बढ़ रहा है। पुराने विवाद और दुश्मनी फिर से तरोताजा हो रही है। यह संघर्ष हिंसक होता जा रहा है। पिछले हफ्ते इलाहाबाद में मुंबई से गांव आए तीन भाइयों का जमीन विवाद के कारण एक साथ हत्या इसका एक उदाहरण है। बहुत सारे जिलों में इस तरह की घटनाओं की ओर गांव तेजी से बढ़ रहा है। बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता ने ऐसे संघर्षों को बढ़ाने में मदद की है।
इतने सारे झंझावातो से जूझ रहे गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के जो सपने बुने जा रहे हैं उसके सामने कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि यह आत्मनिर्भरता व्यक्ति सापेक्ष ना होकर समाज सापेक्ष है और यह तभी संभव है जब उस समाज (गांव समाज) में परस्पर सद्भाव और सहयोग हो।
गांव की आत्मनिर्भरता सिर्फ साधनों की उपलब्धता या प्राप्ति पर नहीं टिकेगी उसके लिए संबंधों की मजबूत भावनात्मक डोर और गहरा व ठोस संवेदनात्मक धरातल भी चाहिए तभी उसमें जीवंतता होगी अन्यथा वह जड़वत होगा। इसी नाते वेबिनार में शामिल प्रतिनिधियों ने गॉव वापस आ रहे कामगारों के प्रति प्यार और सहयोग की भावना के साथ उनकी परेशानी और पीड़ा के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर विशेष जोर दिया। इसके लिए अपेक्षित सुविधाओं के अभाव के बावजूद स्थानीय स्तर पर समुदाय को ही संवेदनशील बनकर उनके अनुकूल भौतिक एवं भावनात्मक परिस्थितियाँ तैयार करनी होगी।
वास्तव में गांव के स्कूल अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर जो कोरनटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें कुछ को छोड़कर ज्यादा तर मे अपेक्षित सुविधाओं का अभाव देखने को तो मिल ही रहा है साथ ही वहां की दिनचर्या भी उबाऊ और नीरस है। जबकि वहां पर रह रहा व्यक्ति मानसिक पीड़ा, सामाजिक उपेक्षा और शारीरिक कष्ट इन सब से गुजर रहा है।
ऐसे में अगर इन सेंटरों पर न्यूनतम सुविधा के साथ-साथ उसके भावनात्मक एवं मानसिक तोष के लिए भी अनुकूल उपाय किए जाएं तो यह नीरसता और उबाऊपन मिट सकता है और उनके लिए सेंटर सुकून का स्थान बन सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की लोक संस्कृति में गीत गायन और नाटकों की एक लंबी एवं समृधि सांस्कृतिक विरासत है। साथ ही खेल कूद और व्यायाम तो उनकी दिनचर्या के हिस्से ही रहे हैं और आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में तो और भी बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं। स्थानीय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार इन सब को जोड़कर सेंटर के माहौल को बहुत ही रूचि पूर्ण और आनंददायी बनाया जा सकता है।
शहर से दूर गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच का अभाव और अव्यवस्था जगजाहिर है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर इसके बचाव के तरीकों की पहचान तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। गांव के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता के बेहतर होने के उदाहरण पहले से ही रहे हैं और इस समय भी वह दिखाई पड़ रहा है। यदि इसे स्थानीय जड़ी बूटियों तथा खान-पान के परंपरागत पौष्टिक तरीकों की उपलब्धता और स्वीकृति बन सके तो गांव में इस महामारी से काफी निजात पाया जा सकता है। बाकी इससे बचाव के राष्ट्रीय स्तर से जो तरीके बताए गए हैं – दो गज की दूरी, साबुन से हाथ धोना और चेहरा ढक कर रखना, इसके प्रति जागरूकता और समझ के प्रयास तो करने ही होंगे।
जहां तक रही राहत की बात तो केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर से जो प्रयास चल रहा है यदि वह सही रूप में गांव तक पहुंच जाए और उसका समुचित वितरण हो जाए तो वह पर्याप्त है। लेकिन इसमें भी काफी अनियमितता व धांधली देखने को मिल रही है। कुछ तंत्र के स्तर पर है तो कुछ स्थानीय स्तर पर।
इसके लिए जिला प्रशासन व स्थानीय शासन अर्थात पंचायत को एक प्रभावी भूमिका निभानी होगी। पंचायत के माध्यम से गांव में बनाई गई निगरानी समितियां ज्यादातर जगहों पर ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, इन्हें भी प्रभावी बनाना होगा।