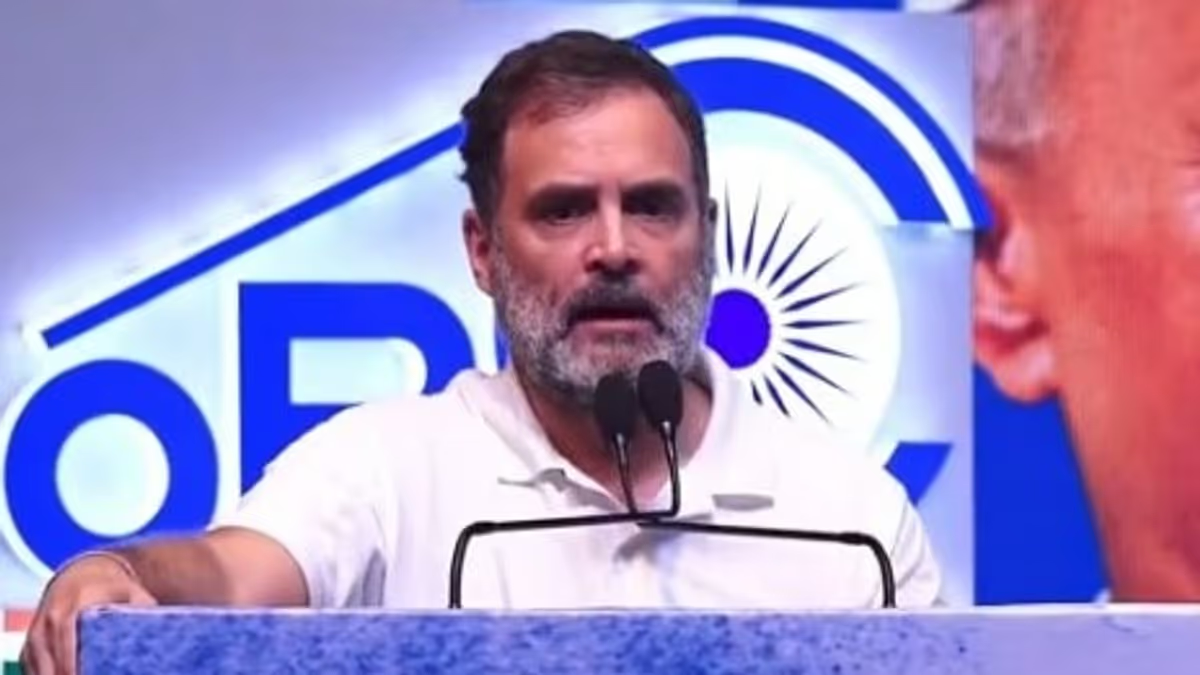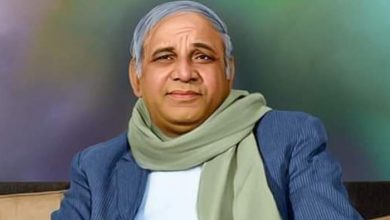क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व के ही जाल में फँस गई है? आंतरिक संकट और नेताओं के किनारे लगाए जाने का विश्लेषण
कांग्रेस नेताओं का पलायन: नेतृत्व, वंशवाद और संगठन का संकट
मीडिया स्वराज डेस्क
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक समय में भारत की राजनीति में अपराजेय मानी जाती थी, आज लंबे समय से गंभीर संकट का सामना कर रही है—चाहे वह संगठनात्मक स्तर पर हो या चुनावी पटल पर। विश्लेषकों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह पार्टी के भीतर असहमति को सुचारू रूप से संभालने और गांधी-नेहरू परिवार के बाहर के प्रभावशाली नेताओं को सशक्त नहीं कर पाने की क्षमता में कमी है।
आलोचकों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाने से लेकर क्षेत्रीय क्षत्रपों की अनदेखी तक, निर्णय-निर्माण की अत्यधिक केंद्रीकरण और वंशवादी आलोचनाओं के बीच, कांग्रेस खुद को एक पुराने ढाँचे में जकड़ी हुई महसूस कर रही है.
वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी
आज के कांग्रेस में एक लगातार चर्चा का विषय है—वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी। जिन नेताओं के पास अनुभव, लोकप्रियता और स्वतंत्र आवाजें हैं, वे लगातार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से दूर होते जा रहे हैं। उदाहरणस्वरूप:
-शशि थरूर—बौद्धिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, फिर भी पार्टी की मूल रणनीति से दूर।
– मनीष तिवारी—‘G-23’ के सक्रिय सदस्य, लेकिन राष्ट्रीय विमर्श का अहम हिस्सा होने के बावजूद बाहर।
– गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल—पार्टी सुधारों की मांग पर उपेक्षा की गई, अंततः पार्टी छोड़नी पड़ी।
– अन्य साइडलाइन हुए नेताओं में** आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चव्हाण, भूपिंदर सिंह हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, संदीप दीक्षित, मुकुल वासनिक और कई नाम हैं।इनमें से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी या संगठन में अप्रासंगिक हो गए।
G-23 विद्रोह: बड़े संकट का प्रतीक
2020 में 23 सीनियर नेताओं के समूह (G-23) ने संगठन में वैचारिक बदलाव, पूर्णकालिक अध्यक्ष और शक्ति के विकेंद्रीकरण जैसी मांगों के साथ पत्र लिखा। इन सुझावों को गंभीरता से लेने के बजाय, इन्हें बागी कहकर किनारे कर दिया गया। परिणामस्वरूप कई दिग्गज जैसे आज़ाद और सिब्बल ने इस्तीफा दे दियाऔर समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्य सभा मेंबर हो गए।
राहुल गांधी का नेतृत्व – सुधारक या सहयोग में असहज?
आलोचना: क्या राहुल गांधी एनजीओ की तरह चला रहे हैं पार्टी?
कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जननेता की बजाय NGO प्रमुख की तरह फैसले करते हैं:
– निर्णय-निर्माण अत्यधिक केंद्रीकृत, खुद के वफादारों के ज़रिए या मुद्दा-आधारित थिंक टैंक से।
– क्षेत्रीय या वरिष्ठ नेताओं से न्यूनतम परामर्श।
– प्रतीकात्मक अभियानों (जैसे भारत जोड़ो यात्रा) पर अत्यधिक बल, मगर जमीनी संगठन या इलेक्टोरल मशीनरी पर कम ध्यान।
इस कारण जमीनी व अनुभवी नेताओं में असंतोष व दूरी बढ़ी है।
कांग्रेस और क्षेत्रीय नेता: पलायन और संकट
कांग्रेस नेतृत्व अक्सर स्थानीय नेताओं को यथोचित सम्मान नहीं दे पाया, जिससे कई मुखर नेता अपनी पार्टियाँ बना कर या विरोधी खेमों में चले गए:
-ममता बनर्जी—कांग्रेस छोड़कर 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई।
– वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी—पार्टी छोड़कर YSR कांग्रेस बनाई, आज आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़।
– शरद पवार—सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाकर NCP बनाई।
– हिमंता बिस्व सरमा—अनदेखी के बाद बीजेपी में जा पहुंचे और आज असम के मुख्यमंत्री हैं।
– नवीनतम उदाहरण**: आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ का पार्टी छोड़ना।
इन नेताओं के जाने के बाद कई प्रदेशों में कांग्रेस का जनाधार तेजी से गिरा:
– बंगाल में तृणमूल ने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया।
– आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के बाद कांग्रेस गायब सी हो गई।
– असम में बीजेपी का उदय और कांग्रेस की सिमटती चुनौती।
परंपरा से वर्तमान तक: नेहरू-इंदिरा से लेकर आज तक केंद्रीकरण
1969 कांग्रेस विभाजन
इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ‘सिंडिकेट’ से खटपट, ‘कांग्रेस (आर)’ और ‘कांग्रेस (ओ)’ में पार्टी बँट गई।
1977 इमरजेंसी के बाद का पलायन
जगजीवन राम, बहुगुणा, मोहन धारिया जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ गए—सख्त नियंत्रण और उपेक्षा की वजह से।
गांधी परिवार का प्रभुत्व: वरदान या बोझ?
सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का साथ-साथ संसद में रहना भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं
सकारात्मक
– नाम और विरासत से भीड़ जुटती है।
– अनुभवी कार्यकर्ताओं में एकता बनी रहती है।
नकारात्मक
– वंशवादी छवि और विपक्षी हमलों को बल मिलता है।
– वैकल्पिक नेतृत्व उभरने नहीं दिया जाता।
– युवाओं और क्षेत्रीय नेताओं में निराशा/भ्रम.
आंतरिक अव्यवस्था के चुनावी असर
1. संगठनात्मक कमजोरी अनुभवी नेताओं के न रहने से राज्यों की जड़ें कमजोर।
2. चुनावी विफलताएँ: हरियाणा, आंध्र, असम, बंगाल जैसे राज्यों में पराजय।
3. युवा मतदाताओं की बेरुखी:पार्टी वंशजों तक ही सीमित दिखती है।
4. गठबंधन की क्षमता कमजोर:क्षेत्रीय नेताओं की अनदेखी से सहयोगी पार्टियों में भी भरोसा घटा है[1][2][10][12][9]।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वरिष्ठ नेता किनारे क्यों होते हैं?
क्योंकि वह नेतृत्व के प्रस्तावों से अलग राय रखते हैं, जिससे उनकी उपेक्षा शुरू हो जाती है।
Q2: कांग्रेस में G-23 क्या था?
2020 में शीर्ष नेताओं ने पार्टी सुधार की मांग रखी, पर प्रतिक्रिया न मिलने पर कई ने पार्टी छोड़ दी[4][5][7]।
Q3: ममता बनर्जी या जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी क्यों छोड़ी?
केंद्रीय नेतृत्व की अनदेखी और राज्यस्तरीय समर्थन न मिलने के कारण उन्होंने अपनी पार्टियाँ बनाईं[3][6]।
Q4: क्या गांधी परिवार का प्रभुत्व कांग्रेस के लिए सही है?
नाम और पहचान मिलती है, लेकिन वंशवादी छवि पार्टी के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए चुनौती बनती जा रही है[15][16][9]।
निष्कर्ष: अब बदलाव की घड़ी
कांग्रेस पार्टी इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर है।
आज भी फैसलों का केंद्रीकरण, क्षेत्रीय और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और गांधी परिवार केंद्रित नेतृत्व पार्टी की सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं।
यदि कांग्रेस खुद को फिर से प्रासंगिक बनाना चाहती है, तो उसे
– निर्णय-निर्माण का विकेंद्रीकरण करना,
– योग्यता और ज़मीनी नेताओं को बढ़ावा देना
– और गांधी परिवार के अलावा भी नेतृत्व को आत्मसात करना होगा।