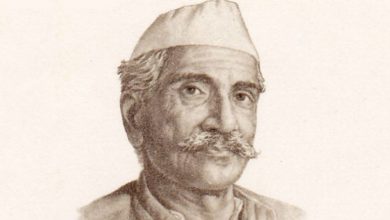होली रंगों का त्यौहार ही नहीं कालगणना और संस्कृति का इतिहास भी है
डॉ आर.अचल पुलस्तेय
भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण त्यौहारों में होली प्रमुख है,जो मूलतःउत्तर भारत से निकलकर विविध नामान्तरण के साथ पूरे दक्षिण एशिया में मनाया जाता है। प्राचीनकाल में मौलिक रूप से यह कालगणना, ऋतुपरिवर्तन, पर्यावरण,स्वास्थ्य और कृषि केन्द्रित त्यौहार था, परन्तु कालान्तर में अनेक पौराणिक,आंचलिक कथायें, किवंदतियां जुड़ने के कारण इसका प्राकृतिक स्वरुप खो गया । आज वैश्विकरण और बाजारवाद के प्रभाव में विद्रूपता के स्तर तक पहुंचने के बावजूद ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों मे इसकी मौलिकता संरक्षित-सुरक्षित है। इसलिए यह कालगणना और संस्कृति का इतिहास भी है। वर्तमान में पर्यावरण और स्वास्थ्य की बढ़ती समस्याओं के बीच इसका मौलिक स्वरुप प्रासंगिक लगता है ।
भारतीय में प्रचलित पारम्परिक कालगणना विधि विक्रम संवत् के अनुसार वर्ष के अंतिम और प्रथम दिन को संयुक्त कर होली के रुप में मनाया जाता है। फाल्गुन मास के पुर्णिमा की रात को होली जला कर,चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात पहले दिन सुबह विविध मीठे, तीखे, पकवानों के साथ,रंग-अबीर, गुलाल,धूल,राख,कीचड़ आदि एक दूसरे पर उन्मुक्त भाव से फेंककर अश्लील, मादक गीत, संगीत, हास-परिहास किया जाता है।विभिन्न अंचलों में इसके मनाने की शैली थोड़ी-बहुत अन्तर के साथ एक जैसी ही है। यह उत्तर भारत व नेपाल का विशिष्ट पर्व है।
वर्तमान में विष्णुपुराण की एक कथा होली के मुख्य आधार के रूप में प्रचलित है। जिसके अनुसार दैत्यकन्या होलिका अपने भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यप के विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करती है। कथा के अनुसार विष्णु की शक्ति से प्रहलाद बच निकलता है और ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने के वरदान के बावजूद होलिका जलकर मारी जाती है। इस मिथक को प्रत्येक वर्ष सांकेतिक रुप से पुनरावृत्ति करके, इसे बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार के पराजय के रुप मे व्याख्यायित किया जाता है,जबकि दूसरे दिन के क्रिया-कलाप से यह मिथक धुंधला हो जाता है।
इस मिथक के अनुसार हिरण्यकश्यप, उसी कश्यप ऋषि के दूसरी पत्नि, दिति के पुत्र हैं जिनसे आदित्यादि देव गण उत्पन्न हुए,अर्थात देवता और दैत्य दोनो सौतेले भाई ही है, होलिका महर्षि कश्यप की ही पौत्री और देवताओं की सौतेली बहन है। यहां सिद्धांतो,विचारधाराओं एवं अधिकार का युद्ध है, होलिका अपने मातृ कुल की विचारधारा के साथ है। इधर दैत्यराज को पराजित करने के उद्देश्य से हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नि का देवताओं द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। प्रसव के पश्चात दैत्यपुत्र प्रहलाद को देव विचारधारा के वातावरण के पालित-पोषित किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरुप प्रहलाद, पिता के विचारों के विरुद्ध हो जाता है। इसी कारण पिता-पुत्र का संघर्ष है। इस कथा के अनुसार मानव भी महर्षिकश्यप की एक पत्नि की संतान है। अंततःहोलिका मानव कुल की भी सौतेली बहन है। ऐसे में यह मिथक एक पारिवारिक संपत्ति के विवाद जैसे है। इसे घृणा और अनंत संघर्ष तक ले जाना राजनैतिक प्रयोजन सा लगता है। ऐसे ही मीमांसा के कारण होलिका दहन के विरूद्ध विचारों का उदय, समय की स्वाभाविक घटना है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मिथकीय सैद्धांतिक युद्ध को घृणा के स्तर तक प्रचारितकर अतिरंजनापूर्ण दुहराव ही आलोचना का कारण है।
इस मिथक से राजस्थान का माड़वाड़ी समाज विशेष प्रभावित रहा है। इनकी परम्परा में किसी मंदिर या गृह परिसर में होलिका की मूर्ति स्थापित की जाती है, सायंकाल महिलायें पूजन करती है, रात्रि में पुरूषों द्वारा होलिका जलायी जाती है इसके पश्चात प्रसन्नता का उत्सव मनाया जाता है। यह परम्परा माड़वाड़ी समाज के विस्थापन के साथ देश के विभिन्न शहरों तक विस्तारित हुई है, इसके प्रभाव में स्थानीय होलिका दहन की परम्परा भी प्रभावित हुई है। इस मिथक का प्रभाव प्रारम्भिक काल में विशेष रुप से भारत के राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में रहा है जो फिल्मों संचार माध्यमो, धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित होता गया, परन्तु ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्र इससे इतर अपनी परम्पराओं पर बने रहे। इस मिथक का संदर्भ तो विस्तारित हुआ पर त्यौहार को अपनी परम्पराओं के अनुसार मनाते रहे। अभी मात्र 25-30 साल पहले तक भोजपुरिया इलाके के ग्रामीण अंचलों मे होली के नाम से यह त्यौहार नहीं जाना जाता था, इस पर्व को उप्र-बिहार में फगुआ कहा जाता था,अब होली शब्द प्रचलन में तो आया है पर होली के बजाय संवत (सम्हत)जलाये जाने की ही परम्परा कायम है।
पुराणों में इस पर्व के संदर्भ में अन्य कथायें भी मिलती है। जैसे शिव-पार्वती-कामदेव की कथा है।जिसके अनुसार देवताओं द्वारा राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित कामदेव ने शिव का ध्यान भंग कर कामजागृत करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर शिव ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिन तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के अभाव मे सृष्टि रुक गयी। सृजन की निरंतरता के लिए देवताओं की सलाह पर कामदेव पत्नि रति ने शिव की उपासना की। जिससे प्रसन्न होकर शिव ने होलिकाष्टक के अंतिम दिन कामदेव को पुनर्जन्म प्रदान किया । इसलिए यह पर्व मदनोत्सव के रुप में मनाया जाता है ।शैव सम्प्रदाय के प्रभाव वाले क्षेत्रो में होली इसी पृष्ठभूमि में मनायी जाती है।
होली के संबंध में कृष्ण से जुड़ी भी एक कथा आती है,जो ब्रज के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति से प्रभावित क्षेत्रों में इस पर्व की पृष्ठभूमि है । बाल्यकाल्य में श्रीकृष्ण को मारने के उद्देश्य से कंसदूती पूतना ने विषाक्त दूध पीला दिया, जिसके कारण उनका शरीर नीला हो गया। कृष्ण सारे बच्चो और गोपियों से अलग वर्ण के दिखने के कारण उदास रहने लगे। मां यशोदा के कहने पर श्रीकृष्ण ने राधा सहित सभी गोपियों-ग्वालबालों के शरीर को नीले रंग से रंग दिया । इसी दिन से राधा, श्रीकृष्ण के प्रेम मे डूब गयी। इसी स्मृति में रंगोत्सव पर्व मनाने की परम्परा विकसित हुई। इसी प्रकार ढुंढी राक्षसी की कथा भी है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा-सूत्र और कथा गार्ह्य-सूत्र, नारद पुराण, भविष्य पुराण, कुमार संभवम् जैसे पुराणों-ग्रंथो की प्राचीन हस्तलिपियों में इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़स्थान में ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है।
शैवागम ग्रंथ,”वर्षक्रियाकौमुदी” में मदनमहोत्सव नाम से इस पर्व का उल्लेख है। जिसके अनुसार प्रातःकाल एक प्रहर संगीत-वाद्य व अपशब्दो के साथ कीचड़ उछाल कर उल्लास मनाते हैं, इसलिए काशी की होली के मायने अगल हो जाते है, यहां शिव के साथ मशान में चिता की राख से होली खेलते हैं। हर्षदेव की रत्नावली में कामदेव का चित्र बनाकर उत्सव मनाने की परम्परा है, कामसूत्र में इसे सुवसंतक पर्व कहा गया।
इन अनेक मिथको से अलग मध्य भारत के आदिवासी समुदाय में पाड़वा पुनाल सावरी के नाम से प्रकृति के नवरस होने और कृषि सत्र बदलने के उत्साह में मनाया जाता है। यहां पलाश को फूलों से रंग बना कर होली खेली जाती है। सामूहिक रुप से पारम्परिक गीत और नृत्य का आयोजन होता है। इस दिन से नये वर्ष का आरम्भ माना जाता है। वास्तव यही इस पर्व का मौलिक स्वरुप है, जिसे आदिवासी समुदाय अभी तक संरक्षित- सुरक्षित किये हुए है।
यह तथ्य भारतीय कालगणना विज्ञान की कसौटी पर शतप्रतिशत खरा उतरता है। भारतीय कालगणना विधि को संवत पंचांग कहा जाता है, ये दो प्रकार के है जिन्हे शकसंवत तथा विक्रम संवत कहते है। विक्रम संवत,शकसंवत के 135 वर्ष बाद आया। जिसका आधार शकसंवत् ही रहा पर इसमें कुछ सूक्ष्म सुधार किये गये। शक के पूर्व कलियुग संवत्,कृष्ण संवत व ऋषिसंवत् का प्रचलित थे। ऋषिसंवत् भारत का सबसे प्राचीन संवत् माना जाता है, इसके होने संकेत विक्रम संवत् से ईसा पूर्व 3076 वर्ष पहले मिलता है। इसकी गणना में पर्वो के आधार पर ही की जाती थी,पर्व का तात्पर्य जोड़(संधि) होता है। इसमें महीनों,दिन का निर्धारण नहीं मिलता है,परन्तु नक्षत्रों की गणना कर मौसम परिवर्तन के संधिकाल का पता चलता था। दो मौसमों के संधिकाल को पर्व के रुप में मनाया जाता था। प्राचीन काल में कृषि के दो ही मौसम वर्षा और शरद काल हुआ करते थे। पानी के अभाव के कारण गर्मी को कृषि का मौसम नहीं माना जाता था। इसलिए पहला पर्व श्रावण में अंतिम पर्व फाल्गुन में माना जाता था, अर्थात फाल्गुन पुर्णिमा कृषिकार्य का अंतिम पर्व हुआ करता था। शक व विक्रम संवत् ऋषि संवत का ही विकसित स्वरुप है। जिसमे भी विधियां साथ-साथ चलती है। सूर्य केन्द्रित तथा चन्द्र केन्द्रित गणना। चन्द्र वर्ष सूर्य से 11 दिन तीन घटी 48 पर कम होता है,इसी को पूर्ण करने के लिए अधिमास की व्यवस्था है।
सौर्य वर्ष में बारह महीनो की गणना मेष,वृष आदि राशियो के अनुसार की जाती है,पृथ्वी सूर्य के परिक्रमण में बारह तारा मंडलो से गुजरती है।इस गति में एक तारा मंडल(राशि) को पार करने में लगभग 30 दिन लगते है,यह एक मास का मानक है, जिस समय जिस राशि से पृथ्वी गुजर रही होती है उसी राशि के नाम पर उस मास का नामकरण किया गया है।इसके अनुसार मेष संक्रांति से वर्ष आरम्भ होकर मीन राशि में समाप्त होता है,मीन मास ही बसंत कहलात है।
चन्द्र वर्ष में सूर्य,पृथ्वी,चन्द्रमा और नक्षत्रों को केन्द्र में रख कर गणना की जाती है, जो सूक्ष्मता के साथ प्रकृति के क्षण-क्षण परिवर्तनो की पहचान में सहायक है,क्योंकि पृथ्वी के दिन-रात व ऋतुओं का कारण चन्द्रमा ही है।इसीलिए बिना किसी यंत्र के जाड़ा-गर्मी-बरसात मौसम और ग्रीष्मादि ऋतुओं का निर्धारण संभव रहा है,यह परम्परा आज भी अविकसित कहे जाने वाले आदिवासी व ग्रामीण अँचलो मे प्रचलित है,जिसके अनुसार फसल चक्र का निर्धारण होता है।
चन्द्र वर्ष की गणना में नक्षत्रों का विशेष महत्व है,चार तारों के समूह को नक्षत्र कहते है।यही नक्षत्रों के चार चरण होते है। लगभग ढाई नक्षत्रों की दूरी को राशि कहते है।इस प्रकार 28 नक्षत्रों में चन्द्रमा और पृथ्वी के परिक्रमण में 12 माह का समय लगता है। इसी के अनुसार प्रकृति के परिवर्तन चक्र को 12 भागो में विभाजित किया गया जिन्हे मास करते है,चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चन्द्रमा एक नक्षत्र के परिक्षेत्र मे 14 से 16 दिन रहता है।इसे अर्धमास या मास पक्ष कहते है,पन्द्रह दिन सूर्य के परोक्ष और पन्द्रह दिन अपरोक्ष रहता है,उसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहा जाता है।इस क्रम में चन्द्रमा पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष एक 365 दिनो मे 28 नक्षत्रो से गुजरता है। पुर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में चन्द्रमा होता है,उसी नक्षत्र के नाम पर मास का नामकरण किया गया है।पर मास की गणना पीछे से की जाती है,इसलिए पुर्णिमा के दूसरे दिन दूसरा मास शुरु हो जाता है,जबकि उस मास के नाम वाली नक्षत्र में चन्द्रमा अंतिम दिन आता है ।
इस क्रम में वर्ष की प्रथम पुर्णिमा चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से जेष्ठ्य़, उत्तराषाढ़ा से आषाढ,श्रावणी से श्रावण, उत्तराभाद्रपद से भाद्रपद, अश्वनी से आश्विन,कृतिका से कार्तिक,पूषा से पौष, मघा से माघ के क्रम में अंतिम पुर्णिमा उत्तरा फाल्गुनी में होने के कारण यह फाल्गुन (फागुन) मास होता है ।
परिक्रमण काल में पृथ्वी का तापक्रम और नमी का क्रम बदलता रहता है,जिसके निर्धारण ऋतुओं के रुप में किया गया है। यह उन नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी व चन्द्रमा के गुजरने के प्रभाव के कारण होता है। यहाँ प्रसंगवश फाल्गुनी नक्षत्र के स्वभाव और पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव की चर्चा करते है।
फाल्गुनी लम्बवत् बड़ी नक्षत्र है जिसके कारण इसे दो भागों, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा पाल्गुनी में बाँट कर गणना की जाती है।
“शतपथ ब्राम्हण” मे फाल्गुनी दो तारे नक्षत्र का वर्णन है। इन्हे अर्जुनी भी कहते है। इसका उल्लेख ऋग्वेद 18. 20. 13 में भी आया है।
फाल्गुनी का शाब्दिक भाव को देखा जाय तो संस्कृत में फाल्गुन का तात्पर्य लालिमा पूर्ण पीला रंग होता है। पूर्वा फाल्गुनी राशि चक्र मे 133।20 से 146।40 अंश के विस्तार क्षेत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कहलाता है तथा 146।40 से 160।00 अंश विस्तार क्षेत्र उत्तरा फाल्गुनी है।
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का देवता भग नामक सूर्य है। स्वामी ग्रह शुक्र, राशि सिंह 13।20 से 26।40 अंश,यह भारतीय खगोल का 11 वाँ उग्र संज्ञक नक्षत्र है। इसके केवल दो तारे है। उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य अर्यमा है। ये संरक्षण, सहायता, अनुग्रह, स्नेह के देवता है।
इस लक्षणा पूर्ण वर्णन से स्पष्ट होता है,कि फाल्गुनी नक्षत्र से प्रभावित फाल्गुन मास में सूर्य की रक्तपित्ताभ किरणें पृथ्वी को भी लाल-पीले रंग में भर देती है,इस समय का तापक्रम वनस्पतियों सहित समतापीय जीवों के लिए सुखद और सर्जनात्मक होता है। प्रकृति सृजन शक्ति अर्थात काम ऊर्जा से भरी होती है।पृथ्वी का वातावरण सौन्दर्य के शिखर पर होता है।जो भुक्त न होने के कारण दैहिक,मानसिक,सामाजिक विकारों का कारण बन सकता है,जिसके विरेचन के लिए इस मास में आनन्दपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति को उश्रृंखलता के स्तर तक गीत-संगीत,शब्द-अपशब्द के माध्यम ले जाने की परम्परा विकसित हुई होगी।
यह संदर्भ भारतीय आयुर्विज्ञान आयुर्वेद की दृष्टि में शरद,शिशिर ऋतु में संचित कफ बसंत ऋतु में उत्तरायण सूर्य के बढ़ते तापक्रम के कारण तरल होने लगता है, जो प्रकुपित होकर ज्वरादि रोग उत्पन्न करता है।इससे बचाव के लिए वमन -विरेचन आदि शोधन कर्म करने का विधान है। इसके पश्चात कच्चे, भूने हुए चना,गेहूँ,जौ आदि के सेवन को कहा गया है, जो होली (फगुआ) को प्रकृति के साथ देह का सामंजस्य स्थापित करने का पर्व सिद्ध करता है।इसमें वमन-विरेचनादि शोधन क्रिया की व्याख्या करते हुए ओशो का कहते है कि होली जैसा त्यौहार मानव जीवन के लिए के परम आवश्यक है,क्योकि इसमें शरीर के साथ मन के विरेचन की भी सुविधा है।इस पर्व के उन्मुक्त,उश्रृंखल व्यवहार सें मन की ग्रंथियाँ भी मिट जाती है।तमाम बंध-प्रतिबंध से मुक्त होकर सहज स्वभाविक प्राकृत हो जाने का अवसर होता है।आरोपित शिष्टाचार मिट जाता है।यह पर्व शरीर और मन को निर्भार कर देता है,आज के प्रतिस्पर्धात्मक तनाव और कुण्ठा के युग में ऐसे त्यौहारो की साप्ताहिक आवश्यकता है । इस प्रकार नवनूतन प्रकृति के साथ एकाकार होने के इस उत्सव को मौलिक रुप से फागुआ या वसंतोत्सव कहना उचित लगता है।
कालगणना के अलावा कृषि के दृष्टि से भी इस पर्व पर एक वर्ष चक्र पूर्ण होता है।ऐसे में गुजरते साल और कृषि चक्र के पूर्णता का उत्सव प्रकृति के रंगीनगी के साथ हो लेने का यह आदिम त्यौहार है जो समय-समय पर विविध पुराणैतिहासिक मिथको, कथाओं से साथ अपना अर्थ व नाम बदलने के बावजूद भोजपुरी जनपदों मे अपने मौलिक स्वरुप को बनाये हुए है।
यहाँ आज भी गाँवो में होलिका के बजाय संवत् (सँम्हत) ही जलाने की परम्परा है । जिसमे वंसतपंचमी के दिन एक हरे बाँस या एरंड के पेड़ में तीसी-जौ का पौधा बाँधकर पान सुपारी के साथ पूजन करके जमीन में गाड़ दिया जाता है । इसी दिन से फगुआ गीत गायन शुरु हो जाता है। यह क्रम विक्रम संवत् के अंतिम दिन पुर्णिमा को जलाने तक चलता है।इसके दूसरे दिन यह उत्सव अपने शिखर पर पहुँच जाता है।इन गीतो में मौसम व प्रकृति के साथ मानवीय संवेदना होती है।भोजपुरी संस्कृति का फगुआ जीवन में बहुत गहराई से रचा-बसा है।भोजपुरी में फगुआ गीत के बाद चैत्र में चैता गीत गाया जाता है,इस क्रम में यहा की गायन शैली हर मौसम के साथ जुड़ी हुई ।संवत् जलाना वर्ष के समापन करने का उत्सव है ।यहाँ उल्लेखनी है कि विक्रम संवत् के अनुसार मास का गणना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से होती है,जबकि शकसंवत् में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मास की गणना की जाती है।ऋषि पंचांग में भी चैत्रकृष्ण प्रतिपदा से ही सवतं आरम्भ होता है,क्योकि संवत् का अतिम दिन फाल्गुन पुर्णिमा है तो स्वभाविक है कि चैत्र कृष्ण ही नये साल का प्रथम दिन होगा ।
इसे स्पष्ट रूप से इस तरह समझा जा सकता है कि पुराना संवत् 2075 पुर्णिमा(20 मार्च2019) को सँम्हत (होली)जलने के साथ बीत गया । 21 मार्च 2019 को नवसंवत् 20176,प्रथम मास चैत्र,कृष्णपक्ष प्रतिपदा पहला दिन हुआ। इस साल की होली(फगुआ) इसी दिन मनायी गयी।इस प्रकार संवत् के पूर्णता का दिन व नये संवत् के आरम्भ को उत्सव के साथ वैदिक काल के पूर्व से मनाया जाता होगा । जो भोजपुरी संस्कृति के साथ दक्षिण एशिया के अनेक अँचलो में आज भी जीवित है ।कालांतर में शकसंवत् को भारत में राष्ट्रीय पंचाग की मान्यता प्रदान की गयी,इसलिए नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष का प्रथम दिन मानकर नववर्ष मनाया जाता है। आगे चल कर पुराण की एक कथा जुड़ती है।चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन व्रह्मा ने सृष्टि की थी इसलिए नववर्ष मनाने की परम्परा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से आरम्भ हो गयी।इसी दिन वासंतिक नवरात्रि भी आरम्भ होता है।इस संबध में दूसरा कारण यह है कि चूँकि मासो का नाम चन्द्र नक्षत्रों के अनुसार रखने की परम्परा है इसलिए चन्द्रोदय के दिन को ही नववर्षारम्भ के रूप में स्वीकार किया गया ।
इस पर्व का होली नामकरण के पीछे वैदिक सूत्र भी मिलते है।कुछ विद्वानों के अनुसार, होला शब्द होलहा से उत्पन्न हुआ है, होलहा या होरहा कच्चे अन्न को अग्नि में भून कर बनाया जाता है।इस समय चना,जौ,गेंहूँ के कच्चे अन्न को भून कर पितरों,देवों को उत्सव के साथ समर्पित करने परम्परा थी,इसीलिए इस पर्व का नाम होला या होली के रुप में जाना जाने लगा।पंजाब में आज भी इसे होला मोहल्ला के नाम से मनाया जाता है।
उड़िसा,बंगाल,असम में इस पर्व पर राधा-कृष्ण की झाँकी निकालकर रंग-अबीर,वाद्य,संगीतमय उत्सव मनाया जाता है,इसे डोल जात्रा कहते है। यहां भी यह त्योहार दो दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन लोग होली के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में मिट्टी की झोपड़ी जलाते हैं। मणिपुर में योसंग के रूप मे होली मनाने की परम्परा है,यह भी नववर्ष का मनाने का पर्व है।महाराष्ट्र में चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी के नाम से होली मनायी जाती है।गोवा में शिमगो मे नाम से वसंत के स्वागत में रंगोत्सव मनाया जाता है,यहाँ माँसाहार और मद्य का प्रयोग होता है,जो इधर कुछ दशको से उत्तर भारत में भी प्रचलन में आ गया है।तमिलनाडु में कमन पोडिगई के नाम से होली मनायी जाती है इसका आधार शिव-पार्वती और कामदेव की कथा है।केरल मे मजुलकुली या उक्कुली के नाम से शान्ति प्रिय तरीके से होली मनायी जाती है।इसी प्रकार कश्मीर,हिमाचल में शैव मिथको पर यह त्यौहार मनाया जाता है।इस क्रम में नेपाल में फागुपुन्निह यानि फागुन पुर्णिमा मनाने की परम्परा है।
सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अलबरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है । भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक मुगल काल की इतिहास की तस्वीरें हैं । अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहाँगीर का नूरजहाँ के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहाँगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहाँ के समय तक होली खेलने का मुग़लिया अंदाज़ ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहाँ के ज़माने में होली को ईद-ए-गुलाबी या आब-ए-पाशी (रंगों की बौछार) कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है।
इसके अतिरिक्त प्राचीन कलाकृतियों, भित्तिचित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हंपी के १६वी शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दम्पत्ति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागिनी ही है। इस चित्र में राजपरिवार के एक दंपत्ति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाया गया है।
साथ में अनेक सेविकाएँ नृत्य-गीत व रंग खेलने में व्यस्त हैं। वे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्तिचित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें 17 वीं शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं और इस सबके मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघुचित्र में राजा को हाथीदाँत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है जिसके गालों पर महिलाएँ गुलाल मल रही हैं।इस प्रकार वसंतऋतु का यह उत्सव भारतीय ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया के कला, साहित्य, संगीत,वास्तु,व्यापार पर अभिन्न सा छाप छोड़ता है ।
प्रकृति के परिवर्तित स्वरुप के साथ तादात्म स्थापित करने का यह उत्सव कालान्तर में अनेकानेक किंवदंतियों,मिथको और बाजार के प्रभाव में रुपान्तरित होकर अपनी मौलिकता खोते हुए होली हुडदंग के स्तर पर पहुँतने के बावजूद प्रकृति के साथ मानव के अभिन्न अवस्था में लाने माध्यम बना हुआ है। जबकि वर्तमान में पर्यावरण व मानसिक प्रदूषण के बढते हुए खतरे को देखते हुए इस पर्व का मौलिक स्वरुप अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।