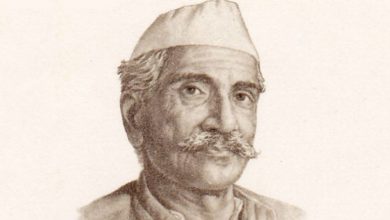राज्यपाल के विशेषाधिकारों की समीक्षा जरूरी
राज्यपाल के विशेषाधिकारों की समीक्षा जरूरी क्योंकि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। बेशक इसमें गलती हमेशा एक पक्ष की नहीं होती, मगर तय रूप से ऐसी स्थिति उन्हीं राज्यों में होती है, जहां केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी दल की सरकार होती है।
ताजा प्रसंग झारखंड का है. मामला एकदम ताजा तो नहीं है. कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने आदिवासी सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन में राज्यपाल की भूमिका समाप्त कर दी थी. भाजपा ने एतराज किया। तब राज्यपाल रहीं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी आपत्ति की। पर सरकार का तर्क है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया जा चुका है, यानी यह असंवैधानिक नहीं है। भाजपा इसे मुद्दा बनाये हुए है. नये राज्यपाल रमेश बैंस ने भी सरकार से पहले स्पष्टीकरण मांगा था. अब अपने स्तर से विधिक सलाह लेकर सरकार को निर्देश दिया है कि वह टीएसी की नियमावली बदले. यह भी कहा है कि सरकार को टीएसी के दो सदस्यों को नामित करने की शक्ति राज्यपाल को देनी होगी. इस पर सरकार का रुख सामने नहीं आया है. मगर जाहिर है कि तकरार जारी है.कुछ दिन पहले तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने त्रिभाषा फार्मूले को, यानी हिंदी की बाध्यता को मानने से इनकार कर दिया है। इस पर राज्यपाल श्री पुरोहित ने कड़ी आपत्ति जतायी। पर इस मामले में तमिलनाडु की भाजपा सरकार के साथ है। तो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है। मगर नीट और हिंदी को लेकर द्रमुक के तेवर तल्ख हैं। उसके मुखपत्र ‘मुरोसोली’ में राज्यपाल की पुलिस की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि डराने वाली शैली पुलिस विभाग में काम करती है, राजनीति में नहीं।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच भी तकरार की स्थिति है। श्री खान का आरोप है कि राज्य की वाम सरकार उनकी सहमति के बिना विश्वविद्यालयों मेंं नियुक्तियां कर रही है। उन्होंने कुलाधिपति की जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है।
इसके पहले विवादास्पद सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किये जाने पर भी श्री खान ने आपत्ति जतायी थी। फिर तीन कृषि कानूनों (जिन्हें अब खुद केंद्र सरकार वापस ले चुकी है) के मुद्दे पर भी ऐसा ही हुआ।
पश्चिम बंगाल में राज्यपाल श्री धनकड़ और राज्य सरकार के बीच ही सतत टकराव की स्थिति बनी हुई है। राज्यपाल पूरी तरह भाजपा नेता की तरह व्यवहार करते दिखते हैं। उधर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी श्री धनकड़ को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति/ केंद्र से राज्यपाल को हटाने की मांग भी की है।
सवाल है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के रहते, राज्यपाल, जो केंद्र द्वारा नियुक्त और उसका प्रतिनिधि होता है, के पास ऐसे अधिकार होने ही क्यों चाहिए? राज्य सरकार के फैसले भले ही राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य और लागू होते हैं, लेकिन कोई राज्यपाल यदि जानबूझ कर और बदनीयती से सरकार के हर फैसले को किसी बहाने लटकाने पर आमादा हो जाये तो? राज्यपाल की विशेष भूमिका की जरूरत तभी पड़ती है, जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो या सरकार का बहुमत संदिग्ध हो जाये। सामान्य स्थिति में राज्यपाल को सरकार के फैसले को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अधिक से अधिक वह एक बार किसी फैसले या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि दोबारा सरकार उस विधेयक को उसी रूप में भेजती है तो राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। हां, नीयत बद हो तो ऐसे विधेयकों या फैसलों को लंबे समय तक लटका कर जरूर रख सकता है। मगर एक लोकप्रिय, चुनी हुई सरकार के फैसलों को इस तरह लटकाने का अधिकार राज्यपाल को क्यों होना चाहिए? विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थाओं की नियुक्तियों में राज्यपाल की रजामंदी अंतिम क्यों होनी चाहिए?
आजादी के बाद करीब दो दशकों तक जब केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थीं, तब सब कुछ ठीक था। उसके बाद स्थिति बदल गयी। केंद्र में जिस दल की भी सरकार रही, उसने राज्यपाल का इस्तेमाल राज्य सरकार को परेशान और अस्थिर करने के लिए किया। मनमाने तरीके से धारा 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए भी। बेशक इस सबकी शुरुआत का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। रामलाल, तपासे और रोमेश भंडारी आदि के कारनामे इतिहास में दर्ज हैं। मगर बीते सात वर्षों में राज्यपाल पद पर आसीन महानुभावों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इन हालात में राज्यपाल के विशेषाधिकारों और भूमिका की समीक्षा जरूरी लगने लगी है। यह भी विचारणीय है कि राज्यपाल का पद क्या इतना अपरिहार्य है? आज के डिजिटल युग में राज्य के हालात जानने के लिए राज्यपाल के रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की अनुशंसा की जरूरत तो वैसे भी नहीं है. तो हर राज्य की राजधानी में राज्यपाल नामक संस्था के खर्चीले तामझाम की जरूरत क्या है? इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता? विचार तो करें। क्या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पद से जुड़े संवैधानिक दायित्व नहीं निभा सकते? यदि राज्यपाल के पास गैरजरूरी विशेषाधिकार न रहें, तो यह आसानी से हो सकता है। राज्य सरकार के जिन फैसलों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है, वे सीधे केंद्र को भेज दिये जायें। अंततः राज्यपाल कोई निर्णय केंद्र या गृहमंत्री की इच्छानुसार ही तो करते हैं।
लगभग यही स्थिति विधानसभा अध्यक्षों की भी हो गयी है। कहने को इन्हें भी दलीय भावना से ऊपर माना जाता है, मगर व्यवहार में अध्यक्ष सरकार के बचाव की मुद्रा में ही रहते हैं। राजनेताओं का राज्यपाल बनना कहीं से गलत नहीं। मगर अपेक्षा की जाती है कि वे दलगत राजनीति और अपने पुराने दल से दूर रहेंगे। प्रारंभ में नेता से राज्यपाल बने लोगों ने बहुत हद तक इसका पालन भी किया। फिर राजभवन पराजित व रिटायर नेताओं की पनाहगाह बनता गया। यहां तक भी ठीक था। बाद में चुनाव हारने पर बने राज्यपाल पद से हटने के बाद या पुनः इस्तीफ़ा देकर चुनाव में कूदने लगे। ऐसे राज्यपाल के लिए जरूरी है कि ‘अपने’ दल के हितों का ख्याल रखें। वे रखते भी हैं। मगर इससे राज्यपाल नामक संवैधानिक संस्था और पद का भारी अवमूल्यन हुआ है। इस कारण भी इस पद के औचित्य और विशेषाधिकारों की समीक्षा जरूरी हो गयी है।नोट- वैसे झारखंड का मामला कुछ विशेष है. इस राज्य का बड़ा हिस्सा पांचवीं अनुसूची के तहत आता है; और उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने, उन पर अमल सुनिश्चित करने का दायित्व और अधिकार राज्यपाल को है. यह और बात है कि शायद ही किसी राज्यपाल ने अब तक पांचवीं या छठी अनुसूची के लिए अपनी और से कुछ किया है. लेकिन अब वही विशेषाधिकार एक बहाना बन सकता है.