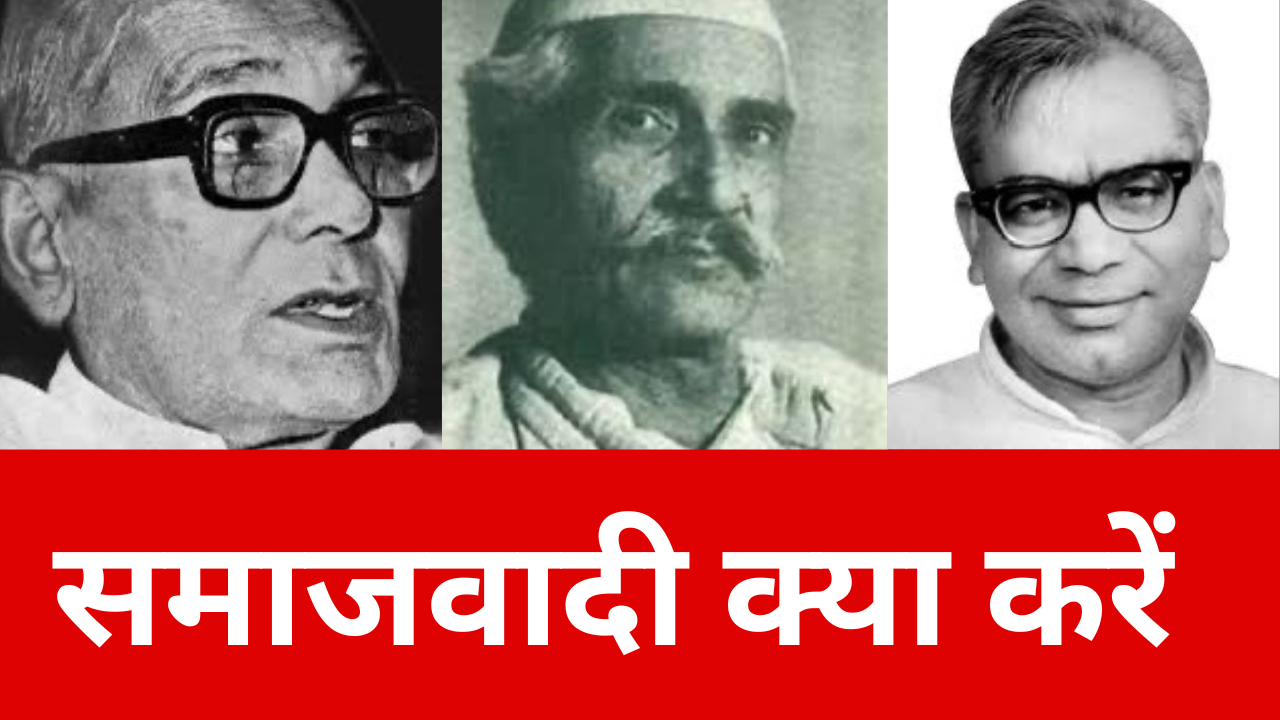आज समाजवादियों को क्या करना चाहिए – प्रो. आनंद कुमार

समाजवादी कार्यकर्ताओं को नयी राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए विचार प्रचार, संगठन निर्माण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, जनमत निर्माण, रचना और संघर्ष के पारंपरिक कार्यों के साथ कम से कम पांच मोर्चों को संभालने की जरूरत है।
हर दौर का अपना कर्तव्य पथ होता है। इसके निर्माण में मूल्यों, सिद्धांतों, नीतियों, कार्यक्रमों और सपनों की भूमिका होती है। इससे र व्यक्ति का युग धर्म निर्धारित होता है। यह तात्कालिक सफलता और असफलता से परे होता है। क्योंकि हर कार्य का तत्काल प्रभाव और अनुकूल परिणाम नहीं होता। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और शीघ्र फूल – फल दे देते हैं।
बड़े सपने साकार होने के लिए ज्यादा समय लेते हैं। जैसे स्वराज का महास्वप्न। इसे सच बनाने में १८५७ से १९४७ के बीच की पीढ़ियों को धीरज के साथ संघर्ष करना पड़ा। कष्ट उठाना पड़ा। रणनीतियों बदलनी पडी। औजार बनाने पड़े। साधन और वाहन विकसित करने पड़े।
आज भारत जैसे देश में समाजवादी सपनों को साकार करने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिस्धितियों की बढ़ती अनुकुलता के बावजूद सतत सक्रियता और धीरज की जादा जरूरत है। क्योंकि राजनीतिक संदर्भ प्रतिकूल है।
संसदवाद का मायाजाल
समाजवादी १९७७ के बाद से ‘संसदवाद’ (चुनाव में विजय) के मायाजाल में उलझ गए हैं। चुनाव हार गए तो समाज में साख का खतरा और चुनाव जीतना है तो समाजवादी सपनों के साथ संबंध विच्छेद। ‘भूखी जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बंट के रहेगी ‘ का नारा मत लगाइए। ‘देशी भाषा में पढ़ने दो, हमको आगे बढने दो ‘ की ललकार की बजाय अपने बच्चों का अंग्रेजी माध्यम के शिशु मंदिरों में दाखिला का रास्ता पकडिए। गांव और गरीब हितकारी दामनीति की लड़ाई से पीछे हटकर ‘कारपोरेट घरानों के लोगों’ को चुनाव प्रबंधन में सलाहकार बनाइए। विना जाति नीति , भाषा नीति और दाम नीति की प्रतिबद्धता के समाजवादी न घर के रहे न घाट के। विनायक बनाने में ढेरों बानर बनाने से जुडते गये।
समाजवादी राह
गांधी के लिए भारत में स्वराज को ग्राम स्वराज के रूप में पंचायत राज के जरिए साकार करना था। हमने इसे संसदीय आंख-मिचौली के जरिए ‘किस्सा कुरसी का’ बना लिया है। लोहिया ने सप्तक्रांति का लक्ष्य दिया और जेल, वोट और फावड़ा के रास्ते पर चलना सिखाया। जेपी की संपूर्ण क्रांति की राह तय करने के लिए युवाओं की आदर्शवादिता और जनता का न्याय बोध का समन्वय चाहिए। दोनों ही दुर्लभ हैं।
वैसे भी औसत व्यक्ति का रचनात्मक काम की सात्विकता में मन नहीं लगता, जेल का रास्ता कठिन है और चुनाव जीतना अमरत्व का राजसी सुख देता है। ‘जबतक सूरज – चांद रहेगा नेता जी का नाम रहेगा’ के नारे से किसे परहेज होगा?
इससे नाराज होने के लिए बुद्ध की अनासक्ति, गांधी का एकादश व्रत, आंबेडकर की ज़िद, जेपी का आत्मविश्वास और लोहिया का कर्तव्यबोध चाहिए।
वैसे भी इस नश्वर दुनिया में समाजवादी नीतियां बहुत थीरज और संकल्प मांग रही हैं जबकि संसदवाद सबसे कम झंझट की राह है। वोट बैंक बनाने में जुटे रहिए, इसी से यह लोक और परलोक दोनों बनेगा और कम से कम सात पीढ़ियों का कल्याण होगा! व्यक्तिवाद और परिवारवाद के दोषों को भूल जाइए। ‘समाजवाद बबुआ धीरे-धीरे आई…..’.
मौजूदा राजनीति में लोकशक्ति और वोट शक्ति
राजशक्ति की दौड़ की राजनीति के लिए वोट बल का महत्व है और चुनाव के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार चाहिए। इसमें जातियों और धर्मों का समीकरण बनाने की मजबूरी है। जाति तोड़ो को स्थगित करके चुनाव के लिए जाति जोड़ो की विवशता है! हर जाति का अपना भौगोलिक दायरा होता है जिससे राष्ट्रीय की बजाय प्रदेश आधारित रणनीति का आकर्षण बढ़ जाता है!! धर्मों का राजनीतिक इस्तेमाल बहुधर्मी राष्ट्रीयता के आदर्श से दूर बहुमत वाले धर्म के वर्चस्ववादी बनने और कम संख्या वाले धर्म अनुयायियों में अलगाववाद की वासनाओं को जगाता है।
राजनीति में चुनाव खर्च को संभालने के लिए अरबपतियों से याराना बढ़ाना पड़ता है। विदेशी अरबपति कंपनियों का हितरक्षक बनना पड़ेगा। चले थे समाजवादी अर्थ व्यवस्था बनाने और बन गये पूंजीवादी ताकतों के पहरेदार! ‘क्रोनी कैपिटलिज्म के साझेदार!! फिर कंचन और कामिनी का अपना आकर्षण और संतति तथा संपत्ति का अपना दबाव होता है।
पांच मोर्चों पर एक साथ काम
फिर भी समाजवादी राष्ट्र निर्माण का कोई विकल्प नहीं है। आज तानाशाही से बचने का यही टिकाऊ उपाय है।
भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए पांच मोर्चों पर एक साथ काम करने की चुनौती है – १. स्वराज निर्माण, २. बहुधर्मी राष्ट्रीयता की पुष्टि, ३. सहभागी लोकतंत्र की रचना , ४. आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता और संपन्नता के युग में प्रवेश, और ५) धर्म निरपेक्ष दलों में चुनाव विभाग की स्थापना।
भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए पांच मोर्चों पर एक साथ काम करने की चुनौती है – १. स्वराज निर्माण, २. बहुधर्मी राष्ट्रीयता की पुष्टि, ३. सहभागी लोकतंत्र की रचना , ४. आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता और संपन्नता के युग में प्रवेश, और ५) धर्म निरपेक्ष दलों में चुनाव विभाग की स्थापना।
प्रोफ़ेसर आनंद कुमार
इसमें आखिरी व्यक्ति के जीवन को स्वराज-संपन्न करना नींव का पत्थर है। इसके लिए हर भारतीय स्त्री -पुरुष को आजीविका का संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई आज एक समाजवादी का पहला मोर्चा है। गरीब को ईश्वर भी रोटी जैसा दिखता है और रोटी में रहता है।
स्वराज यात्रा में अभी तक कौन हाशिए पर हैं? बाल श्रमिक (५ करोड़), विकलांग ( ७ करोड़), वृद्ध स्त्री – पुरुष (७ करोड़), विमुक्त जाति और जनजातियां (१० करोड़) और स्त्री – निर्भर परिवार के सदस्यों (१५ करोड ) का ‘वंचित भारत’ के उल्लेखनीय अंश के रुप में स्वराज यात्रा के हाशिए पर होना हमारे लिए सरोकार का मुद्दा होना चाहिए। इनके स्वास्थ्य, शिक्षा , आजीविका और नागरिक अधिकारों की समस्याओं के समाधान से जुड़ने पर हमारा समाजवादी होना सार्थक होगा।
भारतीय संस्कृति में ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की महिमा का महत्व है। यह राष्ट्रीय आंदोलन की ऊर्जा से बहुभाषी, बहुजातीय और विकेंद्रीकृत संघ के रूप में विकसित हो रही है। लेकिन धार्मिक एकरुपता के समर्थकों की उग्रता ने पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में धार्मिक कट्टरवाद के दुखद
परिणामों की अनदेखी करते हुए ‘हिंदुत्व’ की बुनियाद पर राष्ट्रीयता को पुनर्गठित करने का असरदार प्रयास किया है। नफ़रत और भय से जुड़े इसप्रयास के पक्ष में खुलकर मतदान होना गैर हिन्दू भारतीय नागरिकों को आशंकित कर रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत और भारतीय संविधान के प्राक्कथन की अनदेखी अलगाववादी शक्तियों के अनुकूल सिद्ध होगा।
इस राष्ट्रीय बिखराव को रोकने की जिम्मेदारी पूरी करके भारतीय राष्ट्रीयता का समाजवादी विमर्श इसे मानवतावादी आधार दे सकता है। इसलिए मुहल्ला और गांव स्तर पर एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने से लेकर जिला स्तर पर खेल-कूद, संगीत, साहित्य, और प्रदूषण निवारण के आयोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
असल में तो इस काम के लिए गांधी की तरह बीडा उठाने वाला चाहिए। गांधी १९३४ में सबकुछ के ऊपर अस्पश्यता निवारण के लिए सैकड़ों सहयोगियों के साथ एकाग्रता से जुट गए् और १९४२ में ‘भारत छोड़ो आन्दोलन*में गिरफ्तार किए जाने तक जुटे रहे।
सोसायटी फॉर कम्यूनल हारमनी , खुदाई खिदमतगार और सर्व सेवा संघ से मार्ग दर्शन लेना चाहिए।
सहभागी लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र संवर्धन की अगली सीढ़ी है। बिना उधर कदम बढ़ाए हम लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह के रुप में विकृत करने के अपराधी माने जाएंगे।
चुनाव वैसे भी करोड़पति राजनीतिज्ञों का बंधक होता जा रहा है। बची-खुची कसर दलों में पनपते परिवारवाद और चुनाव में बढ़ते अपराधियों की हिस्सेदारी ने पूरी कर दी है।
हम सांप – छछूंदर की दुविधा में फंसे हुए हैं। लोकतांत्रिक होने के नाते चुनाव से बाहर जाने की संभावना नहीं है। समाजवादी होने के कारण लोकतंत्र का पूंजीपतियों द्वारा अपहरण स्वीकार नहीं किया जा सकता।
दलों में इस महादोष के बारे में उदासीनता है। लोक समिति से लेकर सिटिजन फार डेमाक्रेसी और यूथ फार डेमाक्रेसी के जरिए सरोकारी बनना और सुधार के लिए अभियान चलाना समाजवाद का तकाजा बन चुका है।
बिना चुनाव सुधार और दलों में सुधार के संसदीय लोकतंत्र के लोक हित रक्षक बने रहने की गुंजाइश नहीं बचेगी।
सामाजिक -आर्थिक व्यवस्था का समता मूलक नवनिर्माण समाजवादी परिवार से नयी कार्यसूची चाहता है। जाति नीति को ‘आरक्षण के रूप में विशेष अवसर ‘ से आगे जाकर अतिपिछड़ों की सुनवाई करने की जरूरत है।
जाति जनगणना, रोहिणी आयोग रपट का प्रकाशन, महिलाओं की हिस्सेदारी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांगों को टालने से समाजवादी परिवार पर प्रभुत्व जातियों का वकील होने का शक पक्का हो जाएगा।
इसी तरह आर्थिक सुधारों में विरासत टैक्स, शहरी संपत्ति पर नियंत्रण, विदेशी कमाई कर , खर्च पर सीमा, कृषि टैक्स लागू करने और खेती के लिए निःशुल्क जल और विद्युत व्यवस्था का समय आ गया है।
संपत्ति संचय के बिगड़ते रूप ( १० प्रतिशत के कब्जे में ७७ प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति और ८० करोड़ को निशुल्क अन्न देना!) की अनदेखी आत्मघाती है। समाजवादी होने का दावा करने वाले इस अभूतपूर्व विषमता पर सिविल नाफरमानी के हकदार हैं।
चुनाव व्यवस्था में कारगर हिस्सेदारी
अंतिम मोर्चा चुनाव व्यवस्था में कारगर हिस्सेदारी का है। क्योंकि चुनाव के दोषों के बावजूद चुनावी हार-जीत बहुत मायने रखती है। चुनाव का व्यवसायीकरण हो रहा है और हर दल के लिए विशेषज्ञ के जरिए प्रबंधन अनिवार्य हो गया है।
मतदाता सूची की निगरानी से लेकर मतदान और मतगणना एजेंट की नियुक्ति तक पूरा चुनावी कर्मकांड कामचलाऊ तरीके से नहीं किया जा सकता है।
हर धर्म निरपेक्ष दल को अपने संगठन में चुनाव विभाग स्थापित करना चाहिए। चुनाव प्रबंधन में समाजवादी कार्यकर्ताओं को विशेष दक्षता हासिल करने की आवश्यकता है।
संक्षेप में यह स्पष्ट है कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को नयी राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए विचार प्रचार, संगठन निर्माण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, जनमत निर्माण, रचना और संघर्ष के पारंपरिक कार्यों के साथ कम से कम पांच मोर्चों को संभालने की जरूरत है। यह समाजवाद का नया तकाजा है।