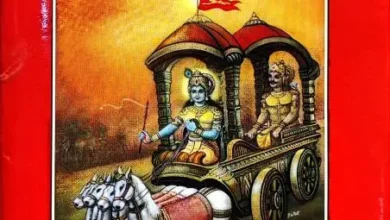स्वधर्म के सहारे ही उन्नति की राह
*गीता प्रवचन दूसरा अध्याय*

प्रस्तुति : रमेश भैया
स्वधर्म के सिलसिले में उपनिषद् में एक सुंदर कथा है।
एक बार देव, दानव और मानव, तीनों प्रजापति के पास उपदेश के लिए पहुँचे।
प्रजापति ने सबको एक ही अक्षर बताया – ‘द’।
देवों ने कहा – “हम देवता लोग कामी हैं, हमें विषय भोगों की चाट लग गयी है। अत: हमें प्रजापति ने ‘द’ अक्षर के द्वारा ‘दमन’ करने की सीख दी है।”
दानवों ने कहा – हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं। हमें ‘द’ अक्षर के द्वारा प्रजापति ने यह शिक्षा दी है कि ‘दया’ करो।”
मानवों ने कहा – “हम मानव बड़े लोभी और धन-संचय के पीछे पड़े हैं, हमें ‘द’ अक्षर के द्वारा ‘दान’ करने का उपदेश प्रजापति ने दिया है।”
प्रजापति ने सभी के अर्थों को ठीक माना, क्योंकि सबने उनको अपने अनुभवों से प्राप्त किया था।
गीता की परिभाषा का अर्थ करते समय उपनिषद् की यह कथा हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
*जीवन –सिद्धांत : (1) देहसे स्वधर्माचरण*
दूसरे अध्यायमें जीवनके तीन महा सिद्धांत प्रस्तुत किये गए हैं – (1) आत्मा की अमरता और अखंडता, (2) देह की क्षुद्रता और (3) स्वधर्म की अबाध्यता।
इनमें स्वधर्म का सिद्धांत कर्तव्य रूप है और शेष दो ज्ञातव्य हैं। पिछली बार मैंने स्वधर्म के संबंध में कुछ कहा ही था।
यह स्वधर्म हमें निसर्गत: ही प्राप्त होता है। स्वधर्म को कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता।
ऐसी बात नहीं है कि हम आकाश से गिरे और धरती पर सँभले। हमारा जन्म होने से पहले यह समाज था, हमारे माँ-बाप थे, अड़ोसी-पडोसी थे।
ऐसे इस प्रवाह में हमारा जन्म होता है।
अत: जिन माँ-बाप की कोख से मैं जन्मा हूँ, उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्मत: ही प्राप्त हो गया है और जिस समाज में मैंने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका धर्म भी मुझे इस क्रमसे अपने-आप ही प्राप्त हो गया है।
सच तो यह है कि हमारे जन्मके साथ ही हमारा स्वधर्म भी जनमता है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उस की पूर्ति के लिए होता है।
कोई-कोई स्वधर्म को पत्नी की उपमा देते हैं और कहते हैं कि जैसे पत्नी का संबंध अविच्छेद्य माना गया है, वैसे ही यह स्वधर्म-संबंध भी अविच्छेद्य है।
लेकिन मुझे यह उपमा भी गौण मालूम होती है। मैं स्वधर्म के लिए माता की उपमा देता हूँ।
मुझे अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा। वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। वह कैसी भी क्यों न हो, अब टाली नहीं जा सकती।
ऐसी ही स्थिति स्वधर्म की है। इस जगत् में स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है।
स्वधर्म को टालनेकी इच्छा करना मानो ‘स्व’ को ही टालने जैसा आत्मघातपन है।
स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अत: यह स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए – यह जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है। *क्रमश:*